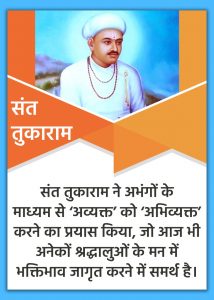
संत तुकाराम, मराठी भाषा के सबसे बड़े भक्त कवि थे। उनकी अनुकरणीय प्रतिभा का पता इसी से चलता है कि उनके अंदर बाहरी दुनिया को आध्यात्म में बदलने की असाधारण क्षमता थी। मराठी साहित्य में तुकाराम का कद अंग्रेजी में शेक्सपियर और जर्मन में गोएथ से कम नहीं है। वह सर्वश्रेष्ठ मराठी कवि थे। जिन्होंने अपनी प्रतिभा, भाषा के साथ-साथ अपने चरित्र से साहित्य और संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
ऐसा कोई दूसरा मराठी लेखक नहीं है जिसने मराठी साहित्य और उसकी संस्कृति को इतना गहरा और व्यापक रूप से प्रभावित किया हो। मराठी कविता संत तुकाराम की शैली के बिना अधूरी है।
मुख्य बातें और उपदेश
पुण्य पऱउपकार पाप ते परपीडा । आणीक नाही जोडा दुजा यासी ॥१॥
सत्य तोचि धर्म असत्य ते कर्म । आणीक हे वर्म नाही दुजे ॥धृ॥
गति तेचि मुखी नामाचे स्मरण । अधोगति जाण विन्मुख ते ॥२॥
संतांचा संग तोचि स्वर्गवास । नर्क तो उदास अनर्गळा ॥३॥
(अच्छाई दूसरों का भला करने में है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना पाप है। इसके अलावा कोई अन्य चीज तुलना के लिए नहीं है। सत्य ही एकमात्र धर्म है (या स्वतंत्रता); असत्य बंधन है, इसके अलावा कोई और रहस्य नहीं है। जबान पर भगवान का नाम आना ही मोक्ष हैं, भगवान की अवहेलना करना ही नाश का कारण है। अच्छे की संगति ही एकमात्र स्वर्ग है, ज्ञानी अगर उदासीन है तो वह नरक के समान है। तुका कहते हैं: इस प्रकार यह स्पष्ट है कि क्या अच्छा है और क्या नुकसानदेह है, लोगों को वह चुनने दो जो वह चाहते हैं।
वेद अनंत बोलिला । अर्थ इतकाचि शोधिला ॥१॥
विठोबासी शरण जावे । निजनिष्ठा नाम गावे ॥धृ॥
सकळ शास्त्रांचा विचार । अंती इतकाचि निर्धार ॥२॥
अठरापुराणी सिद्धांत । तुका म्हणे हाचि हेत ॥३॥
( सागर जैसे वेदों का सार यह है: भगवान की शरण लो और पूरे दिल से उनका नाम दोहराओ। सभी शास्त्रों के योगों का परिणाम भी एक ही है; तुका कहते है: अठारह पुराणों का सार भी यही है।)
जे का रंजले गांजले । त्यासी म्हणे जो आपुले ॥१॥
तोचि साधु ओळखावा । देव तेथेचि जाणावा ॥धृ॥
मॄदु सबाह्य नवनीत । तैसे सज्जनाचे चित्त ॥२॥
ज्यासी आपंगिता नाही । त्यासी धरी जो हॄदयी ॥३॥
दया करणे जे पुत्रासी । तेचि दासा आणि दासी ॥४॥
तुका म्हणे सांगू किती । तोचि भगवंताची मूर्ती ॥५॥
( उस सच्चे मनुष्य को पहचानों ,जो संकट में पड़े लोगों की मदद करता है। यह जान लो कि ईश्वर ऐसे ही सच्चे इंसान के हृदय में निवास करता है। उसका हृदय सज्जनता से भरा होता है। ईश्वर उसे ही प्राप्त होता है जो त्याग करता है। ऐसा व्यक्ति अपने सेवकों से उसी तरह स्नेह करता है जैसे वह अपने बच्चों को प्रेम करता है। तुकाराम कहते हैं: इससे ज्यादा और बताने की क्या जरूरत है? ऐसा मनुष्य देवत्व का अवतार है)
(स्रोत- तुकाराम गाथा)
- जब कोई दर्पण में देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी और को देख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वह स्वयं को देख रहा है।
- मैं वह शाखा हूं जो नदी में विलीन हो गया है।
- मेरा देश अब संपूर्ण ब्रह्मांड है।
- मुक्ति को बाजार में नहीं खरीदा जा सकता है,न ही इसे जंगल या जंगल में भटक कर प्राप्त किया जा सकता है।
- बहुत ज्यादा धन भी मुक्ति नहीं दे सकता है, न ही इसे ऊपरी या किसी दूसरी दुनिया में पाया जा सकता है।
- तुका कहते हैं, जीवन की कीमत पर ही मुक्ति हासिल की जा सकती है।
(स्रोत : Ranade, R. D. Mysticism in India. Albany, NY. SUMY Press, 1983, pp. 303, 312, 320, 339, 349. )
- वह जो चलते समय परमेश्वर के नाम का उच्चारण करता है, उसे हर कदम पर बलिदान करने का साहस रखता है।
- उसका शरीर तीर्थ बन जाता है।
- वह हर काम करते समय परमेश्वर का नाम दोहराता है वह
- हमेशा पूर्ण शांति पाता है।
- .वह काम करते समय भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसे उपवास की योग्यता प्राप्त होती है, भले ही उसने अपना भोजन लिया हो।
- .यहां तक कि अगर कोई पूरी पृथ्वी समुद्र के साथ दान में दे डाले तो भी भगवान का नाम दोहराने जैसा कुछ नहीं है।
- ईश्वर के नाम की शक्ति से किसी को पता चल जाएगा कि क्या नहीं जाना जा सकता है,
- जो नहीं देखा जा सकता है वह भी देखेगा,
- . जो बोला नहीं जा सकता, उसे भी वह बोलेगा
- .जो नहीं मिल सकते, उससे भी मिलेगा
- .तुका कहते हैं, भगवान के नाम को दोहराने से अतुलनीय लाभ मिलता है।
(Source : Ranade, R. D. Mysticism in India. Albany, NY. SUMY Press, 1983, pp. 303, 312, 320, 339, 349)
- संत ईश्वर के साथ इतना एकाकार हो जाता है कि ईश्वर और संत में अंतर करना असंभव हो जाता है।
- आलिंगन गले से मिलता है।
- शरीर से शरीर एकरूप होता है।
- शब्द शब्दों से घुल-मिल जाते हैं।
- आंखें आपस में मिल जाती हैं।
- मैंने अपनी कमर कस ली है, और जीवन के सागर को पार करने का एक रास्ता खोज लिया है।
- बड़े और छोटे, महिलाएं और पुरुष यहां आओ यहां आओ
- कुछ मत सोचे; कोई चिंता नहीं है।
- मैं आप सभी को दूसरे किनारे पर ले जाऊंगा।
- भगवान के एकमात्र निशानी के वाहक के रूप में आओ
- उसके नाम के साथ आपको ले जाने के लिए आया हूं।
(Source : Ranade, R. D. Mysticism in India. Albany, NY. SUMY Press, 1983, pp. 303, 312, 320, 339, 349.)
विस्तृत जीवन परिचय
संत तुकाराम ( वर्ष1609-1650) का जन्म पुणे के पास एक छोटे से गांव देहू में हुआ था, जो संत ज्ञानेश्वर के संजीवनी-समाधि, आलंदी से बहुत दूर नहीं था। दोनों शहर इंद्रायणी नदी के तट पर स्थित हैं। संत तुकाराम के जन्म और मृत्यु का वर्ष 20 वीं सदी के विद्वानों के बीच शोध का विषय है। संत का तुकाराम का जन्म कनकर और बोलोबा मोरे के घर हुआ था और विद्वान उनके परिवार को कुनबी जाति का मानते हैं। उनका बचपन बड़े आराम और विलासिता में बीता, क्योंकि परिवार समृद्ध था। उन्होंने शिक्षा की शुरुआत पंतोजी (गैर-औपचारिक ग्राम से की थी। वर्णमाला को समझाने के लिए प्रत्येक अक्षर को कंकड़ का रूप दिया गया था।
तुकाराम के परिवार के पास कृषि और व्यापार के साथ-साथ उधार देने का व्यवसाय था। उनके पिता हिंदू देवता विष्णु के अवतार विठोबा (वैष्णव) के भक्त थे। वह जब 17 साल के थे तो उनके माता-पिता की मृत्यु हो गई। उनकी पहली पत्नी का नाम रूखमा बाई था और एक बेटा था, जिसका संतू था। शुरू में तुकाराम ने अपने पिता के व्यवसाय में अच्छा हाथ दिखाया, लेकिन वह घाटे में चला गया। एक भयानक अकाल में पत्नी रूखामा और उनके बड़े बेटे की मौत हो गई। उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय में शुरू में अच्छा काम किया, फिर विपत्ति आई, और धीरे-धीरे वह घाटे में चला गया।
व्यवसाय को दोबारा शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत की, पैसे उधार लिए और दूसरे व्यवसायों में भी हाथ आजमाया लेकिन वह दिवालिया हो गए। ग्राम सभा ने उन्हें अपमानित किया और उनका महाजन पद भी छीन लिया। मृत्यु और व्यापक गरीबी का तुकाराम पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो सह्याद्रि श्रेणी (पश्चिमी घाट)पर चिंतन करने चले गए और बाद में उन्होंने “उन्होंने अपने स्वयं के साथ विचार-विमर्श किया” लिखा। तुकाराम ने फिर से शादी की, और उनकी दूसरी पत्नी का नाम अवलाई जीजा बाई था।यह सामान्य बात है कि अकाल का सबसे अनुचित लाभ व्यापारी और साहूकार उठाते हैं। आज भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं, जो जानबूझ कर ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं, जिससे वह नापाक इरादों को पूरा कर सके।
हालांकि, तुकाराम ऐसे हृदयहीन व्यापारी नहीं थे, जो अकारण दुख सह रहे लोगों से जबरन अपने कर्ज की वसूली करे। इसके विपरीत, अपने व्यक्तिगत दुःख को एक तरफ रखते हुए, वह अकाल पीड़ित लोगों की उदारता से मदद करने के लिए आगे आए। वह एक दोहे में कहते हैं कि बहुत खर्च हो चुका था। कुछ चीजें ही बची थी, जो ब्राह्मणों और भिक्षा मांगने वालों को दे दिया । हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि (जैसा कि आमतौर पर किया जाता है) खुद को जानबूझ कर दिवालिया कर लिया।
तुकाराम ने जिस तरह अपने प्रियजनों और करीबियों के शोक का सामना किया वह बहुत साहस भरा परिचय था। वह इन कष्टों से दूर नहीं भागे। वह कभी पलायनवादी नहीं था। वह दिन-प्रतिदिन के कार्य में विजय पाने के इच्छुक थे। इन सभी विपत्तियों ने उन्हें धन, मानवीय स्थिति और मानवीय संबंधों का मूल्यांकन करने का मौका दिया। वह सत्य की खोज में भामनाथ पर्वत चले गए। उनका दृढ़ संकल्प था वह तब तक वापस नहीं आएंगे, जब तक सत्य को समझ नहीं लेंगे। जंगली जानवरों ने उन पर हमला किया और सांपो ने परेशान किया लेकिन तुकाराम का निश्चय अडिग रहा। उनकी तपस्या जब पंद्रहवें दिन पहुंची तो उन्हें अनन्त सत्य का का ज्ञान मिला।
अकाल की भयावहता और बार- बार असफलता मिलने के बाद, तुकाराम अपने परिवार के देवता विठ्ठल की भक्ति में लीन हो गए। तुकाराम का परिवार पीढ़ियों से वरकरी का भक्त था। उनके पूर्वजों में से एक, विश्वंभर, भगवान विठ्ठल से इतना आकर्षित थे कि वह हर एकादशी पर यानी महीने में दो बार 250 किलोमीटर की दूरी तय कर पंढरपुर जाते थे। अपने भक्त के इस भक्ति को देखकर भगवान विठ्ठल और रुक्मिणी, देहू में ही दो काले पत्थर की मूर्तियों में प्रकट हुए और उसी के बाद तुकाराम के पैतृक देवता बन गए।
उन्होंने अपने बाद का जीवन भक्ति, सामुदायिक कीर्तन और अभंग कविता की रचना में बिता दिया।तुकाराम के आध्यात्मिक गुरु बाबाजी चैतन्य थे, जो स्वयं 13 वीं शताब्दी के विद्वान ज्ञानदेव की चौथी पीढ़ी के शिष्य थे।
संत तुकाराम और छत्रपति शिवाजी
महान हिंदू राजा शिवाजी के गुरु, संत समर्थ रामदास ने उन्हें तुकाराम से मिलने के लिए कहा था। शिवाजी ने तुकाराम से मिलने का फैसला किया। एक बार में ही उन्हें तुकाराम की महानता का अहसास हो गया । वह बार-बार तुकाराम के पास जाने लगे। एक बार जब शिवजी संत तुकाराम से मिलने गए, तो उन्होंने संत को महंगे कपड़े, आभूषण और सोने के सिक्के दिए। संत तुकाराम ने राजा के उपहार को लेने से इनकार कर दिया और कहा,इस खजाने का क्या उपयोग है (संत के लिए), हम केवल भगवान विठोबा को चाहते हैं। आपके उपहार आपकी उदारता को दर्शाता है, लेकिन, हमारे लिए, यह कंकड़ जैसा है। हमारे लिए धन गाय के मांस के समान अवांछनीय है। उन्होंने शिवाजी को भगवान विठोबा की भक्ति करने और उनका सेवक बनने की सलाह दी।
शिवाजी संत तुकाराम की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उनके भक्त बन गए। शिवाजी को उनकी ओर आकर्षित होता देख, संत ने उन्हें और उनके सैनिकों को जीवन जीने के तरीके को सिखाया। उन्होंने कहा कि मुझे संसार को उपदेश देना चाहिए, लेकिन आपको क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। शिवाजी संत तुकाराम की सलाह का सार समझ गए। और उन्होंने हिंदू महिमा, सुशासन और सांस्कृतिक उत्थान का शासन स्थापित किया। कई कहानियां प्रचलित हैं जो बताती हैं कि कैसे संत तुकाराम ने शिवाजी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आध्यात्मिक पृष्ठभूमि प्रदान की उनकी आपस में हुई बातचीत अध्ययन का विषय है। एलेनोर ज़ेलियोट कहते हैं कि तुकाराम सहित भक्ति आंदोलन के कवि शिवाजी के उदय में अहम स्थान रखते हैं ।
संत तुकाराम का महात्मा गांधी पर प्रभाव
महात्मा गांधी ने 20 वीं शताब्दी की शुरूआत में जब वह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपने अहिंसक आंदोलन के लिए यरवदा सेंट्रल जेल में कैद किए गए थे। उस समय उन्होंने उपनिषद, भगवद गीता के साथ तुकाराम की कविता और अन्य भक्ति आंदोलन के कवि-संतों की कविताओं को पढ़ा और अनुवाद किया। संत तुकाराम ने अपनी अंतिम सांस वर्ष 1649 या 1650 में ली।
तुकाराम का साहित्य में महत्व
तुकाराम गाथा, संत तुकाराम के कार्यों का मराठी भाषा में संकलन है, जो संभवतः वर्ष 1632 और 1650 के बीच रचा गया है। जिसे अभंग गाथा भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा का मानना है कि इसमें कुछ 4,500 अभंग शामिल हैं, लेकिन आधुनिक विद्वानों ने उनमें से अधिकांश की प्रमाणिकता पर सवाल उठाया है। कविताओं में उन्होंने मानवीय भावनाओं और जीवन के अनुभवों, कुछ आत्मकथाओं और आध्यात्मिक संदर्भों को स्थान दिया। उनकी प्रवरितियों में संघर्षों की चर्चा है। जिसमें जीवन, परिवार, व्यवसाय और निवृति के लिए जुनून – त्याग करने की इच्छा, व्यक्तिगत मुक्ति के लिए सब कुछ पीछे छोड़ना, मोक्ष आदि का वर्णन है।
तुकाराम की शिक्षाएं
मनुष्य जीवन में तब तक सुख प्राप्त नहीं करेगा जब तक उसके जीवन में भगवान के लिए कोई जगह नहीं हो होगी। कोई भी खुशी तब तक संभव नहीं होगी जब तक इंसान नश्वर भगवान को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएगा। मेरे अनुभव को देखो। मैंने ईश्वर को अपना बना लिया और उसे जब भी और जहां भी मैंने उसे रखा, उसने मेरे सवालों के जवाब दिए।’ यह नियति थी जिसने तुकाराम के सांसारिक बंधनों को खत्म कर दिया। यह ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से था कि उन्होंने एक महान आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की। नियति नियंत्रण में नहीं थी,लेकिन भक्त के प्यार को भगवान को मानना ही पड़ता है।
भक्त का प्यार पट्टे की तरह है, हरि वहीं जाता है, जिधर भक्त जाता है। ‘ ऐसा दिव्य प्रेम उसी के स्मरण से प्राप्त होता है। हमें आपका नाम सुनाना चाहिए, आपको हमें अपना प्यार देना चाहिए। जहां भी संत रहते हैं वहां प्रेम प्रचुर मात्रा में रहता है। प्रेम का लेन-देन भक्त और भगवाने के संबंधों का हिस्सा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो विद्वानों और जानकारों सहित किसी को भी भक्ति द्वारा प्रदान किए गए आनंद का कोई पता नहीं चलता। यह ऐसा प्रेम है जो पूरे समाज को एक साथ बांधता है और सभी मतभेदों और भेदभावों को दूर करता है। यह ऐसा प्रेम है जो मनुष्य के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाता है। यह अलौकिक प्रेम सर्वशक्तिमान को याद करने और संतों के साथ जुड़ने से प्राप्त होता है। यह दुःख को सुख में बदल देता है वास्तव में यह जीवन को ही बदल देता है।
सलाह
किसी को सलाह देने का कोई मतलब नहीं, अब केवल सलाह यह है कि अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाओ। अगर कोई विचार नहीं मिलता है तो इस प्रकार तुका गाते हैं, आपका मूल्यवान जीवन बेकार हो जाता है यही सलाह है। तुका का कहना है कि जो आपके हितों का ध्यान रखता है, उसके अलावा कौन सिखा सकता है। अपने माता-पिता को खुश रहने से अच्छा क्या है। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले पुत्र और पुत्रियों के पवित्र व्यवहार से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गीता और भागवत को सुनना चाहिए और ध्यान को भगवान विठोबा पर केन्द्रित करना चाहिए। तुका का कहना है कि स्वच्छ और साफ दिमाग के साथ चिंतन करने के बहुत फायदे हैं।
संतों के साथ का असर
बुरे लोगों की संगति कभी न रखें, हमेशा संतों की संगति में रहने का प्रयास करें। वंचित और दबे-कुचले का उत्थान संतों की महानता है, इसलिए संतों के पीछे बुरे और पिछलग्गू को रोकना चाहिए। केवल ईमानदार माध्यम से धन कमाएं और इसे निराकार भाव से इस्तेमाल करें। यह देखा गया है कि तुकाराम की शिक्षाओं का केंद्र अच्छी सोच, त्रुटिहीन अलगाव और समानता है। मानव कल्याण के लाभ के लिए संदेशों का प्रसार करते हुए उन्होंने एक कुदाल को कुदाल कहने में कभी संकोच नहीं किया।
सामाजिक सुधार
तुकाराम ने अपने शिष्यों और भक्तों में लिंग या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। उनके भक्तों में से एक बहिना बाई, एक ब्राह्मण महिला थी, जिसे भक्ति मार्ग और तुकाराम को अपना गुरू चुनने पर अपने पति के क्रोध और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। तुकाराम ने सिखाया, रानाडे कहते हैं कि “जाति के गौरव ने कभी किसी आदमी को पवित्र नहीं किया”, “वेद और शास्त्रों ने कहा है कि भगवान की सेवा के लिए, जाति मायने नहीं रखती”, यह भगवान की बात है” । एक व्यक्ति जो भगवान से प्यार करता है, वह वास्तव में एक ब्राह्मण है; उसके पास शांति, संयम, करुणा और साहस ने अपना घर बना लिया है। हालांकि 20 वीं सदी के शुरूआत में विद्वानों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या तुकाराम ने खुद जाति को बंधन को स्वीकार किया। क्योंकि उनकी बेटियों ने अपनी ही जाति के पुरुषों से शादी की। फ्रेजर और एडवर्ड्स ने साल 1921 में तुकाराम पर अध्ययन करते हुए कहा कि यह जरूरी नहीं है, क्योंकि पश्चिम में लोग आमतौर पर स्वयं के आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अपने घर के लोगों की शादी करना पसंद करते हैं।
डेविड लोरेनजेन कहते हैं कि वरकारी सम्प्रदाय की स्वीकार्यता में तुकाराम के प्रयास और सुधार की भूमिका भारत भर में भक्ति आंदोलनों में पाए जाने वाले विविध जाति और लिंगों को शामिल करने का अनुसरण करती है। वरकरी संप्रदाय परंपरा में माना जाता है के तुकाराम शूद्र वर्ण के नौ गैर ब्राह्मणों में से एक थे । बाकी में दस ब्राह्मण थे। और दो संत ऐसे जिनकी जाति की उत्पत्ति अज्ञात है। इक्कीस में से चार महिलाओं को संत के रूप में मान्यता है। जिसमें दो ने ब्राह्मण और दो ने गैर-ब्राह्मण परिवारों में जन्म लिया था। वरकारी-सम्प्रदाय में हुए सामाजिक सुधारों के अनुसार तुकाराम के प्रयासों को ऐतिहासिक संदर्भ और समग्र आंदोलन के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।
संदर्भ:
Abbott, J. A & Gobole N.R (1933) Indian Saints , Motilal Banarasidas, Delhi
John Hoyland (1932), An Indian Peasant Mystic: Translations from Tukaram, London: Allenson,
Wilbur Deming (1932), Selections from Tukaram, Christian Literature Society,
Prabhakar Machwe (1977), Tukaram’s Poems, United Writer,
Dilip Chitre (1970), The Bhakta as a Poet: Six Examples from Tukaram’s Poetry, Delos: A Journal on and of Translation, Vol. 4, pages 132-136
Fraser, James Nelson; Rev. JF Edwards (1922). The Life and Teaching of Tukārām. The Christian Literature Society for India, Madras.
