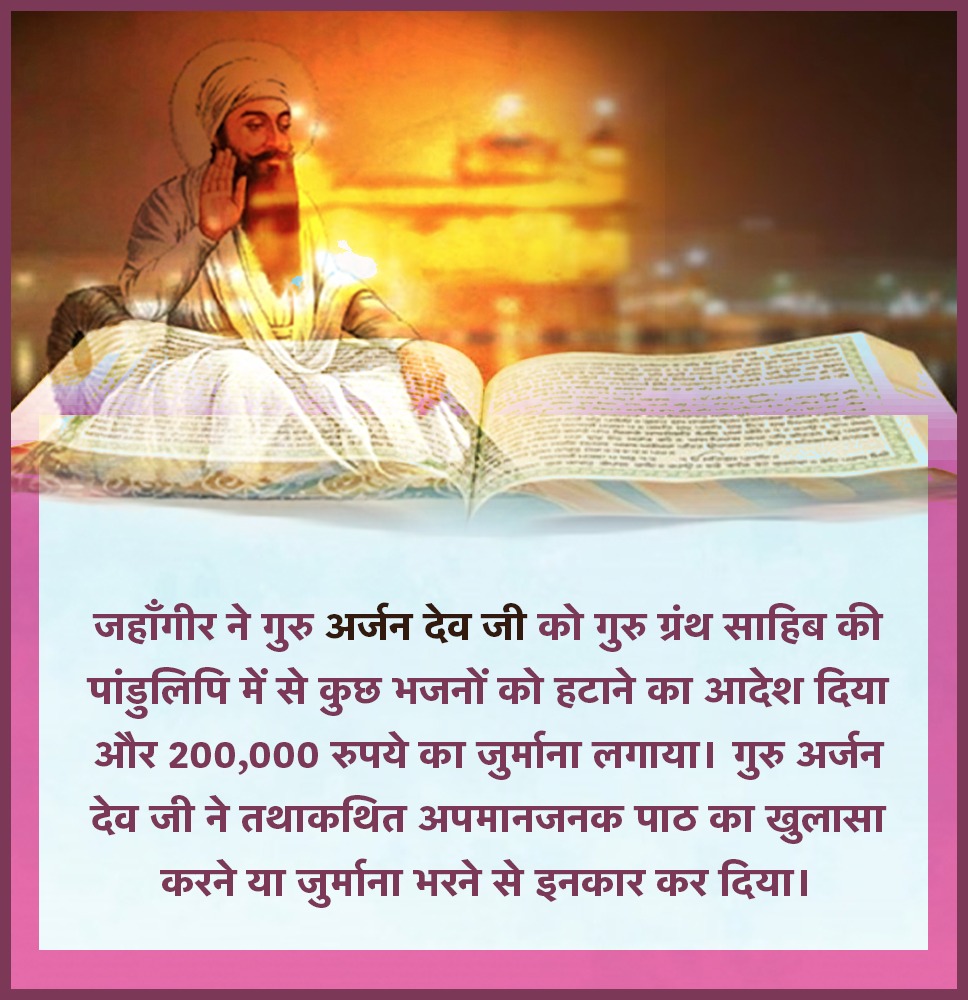भारत ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की धरती है। यहाँ वेद, गीता, रामचरितमानस जैसे कई धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। विश्व के प्रमुख धर्मग्रंथों में सबसे नवीन है गुरु ग्रंथ साहिब। न केवल आकार की दृष्टि से, बल्कि सामग्री के लिहाज से भी यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें ईश्वर और मोक्ष के अलावा जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में व्यक्ति को मार्गदर्शन मिलता है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब समूची मानव जाति का साँझा गुरु है। गुरु अर्जुनदेव ने इस महान् ग्रंथ का संकलन और संपादन करते समय ‘खत्री, ब्राह्मण, सूद, वैस, उपदेसु चहुँ वर्णा कउ साँझा’ के धार्मिक समता तथा समन्वयकारी उद्देश्य को सामने रखा। चौदह सौ तीस पृष्ठ वाले इस विशाल और महान आध्यात्मिक ग्रंथ को धूमधाम और पूर्ण धार्मिक मर्यादा के साथ हरिमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर, अमृतसर) में स्थापित किए जाने (सामान्य सिख शब्दावली में जिसे प्रकाश करना कहते हैं) की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। आदि ग्रंथ को एक जुलूस की शक्ल में हरिमंदिर साहिब ले जाया जा रहा था। गुरु अर्जुनदेव के निष्काम सेवक बाबा बुड्डाजी ने आदि ग्रंथ को अपने सिर पर उठा रखा था। उनके पीछे सैकड़ों श्रद्धालु सतनाम वाहेगुरु का जाप और आदि ग्रंथ पर फूलों की वर्षा करते हुए चल रहे थे। हरिमंदिर साहिब के भीतर पहुँचकर पवित्र ग्रंथ को मंजी साहिब (छोटा खटोला) पर सम्मान के साथ रखा गया और उसपर सुंदर रूमाले (वस्त्र) सजाए गए। इसके बाद गुरु अर्जुन तथा अन्य सभी श्रद्धालु आदि ग्रंथ को नमन करके उसके समक्ष श्रद्धा के साथ बैठ गए। गुरु अर्जुन ने बाबा बुड्डाजी को आदि ग्रंथ में से हुक्मनामा (पवित्र ग्रंथ में से एक पद्य पढ़ना) लेने के लिए कहा। बाबा बुड्डाजी ने आदि ग्रंथ को खोलकर प्रथम हुक्मनामा लिया तो निम्नलिखित शबद (पद्य) आया-
‘संता के कारजि आप खलोइआ
हरि कंमु करावणि आइआ राम…’।[1]
इस प्रकार आदि ग्रंथ का हरिमंदिर साहिब में धार्मिक मर्यादा के साथ प्रथम प्रकाश हुआ। बाबा बुड्डाजी को गुरु अर्जुन ने ग्रंथ साहिब का पहला ग्रंथी नियुक्त किया। आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुनदेव हमेशा ऊँचे आसन पर सुशोभित करते और स्वयं नीचे जमीन पर सोते। इतना अधिक सम्मान देते थे, वे इस पवित्र ग्रंथ को।
गुरु ग्रंथ साहिब की रचना के पीछे गुरु अर्जुनदेव का उद्देश्य संसार की आध्यात्मिक भूख को शांत करना और उसका उद्धार करना था। राग मुंदावणी में रचित अपने निम्नलिखित शब्द (सबद) में गुरुजी बताते हैं –
थाल विचि तिनि वस्तु पईओ, सतु संतोखुविचारो ।
अमृत नाम ठाकुर का पइओ, जिसका सभसु अधारो ।
जे को खावै जे को भुंचे, तिसका होइ उधारो ।
ऐह वस्त तजी नह जाई, नित नित रखु उरिधारो ।
तम संसारु चरन लग तरीऔ, सभु नानक जी ब्रह्म पसारो ॥[2]
अर्थात् मैंने विश्व की आध्यात्मिक भूख की शांति के लिए गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में एक बहुमूल्य थाली में तीन वस्तुएँ परोसकर रख दी हैं। ये वस्तुएँ हैं — सत्य , संतोष तथा प्रभु के अमृत नाम का विचार। जो भी प्राणी इन वस्तुओं को खाएगा और पचाएगा (यानी गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को पढ़ेगा तथा जीवन में उसपर अमल करेगा) उसका उद्धार होगा (जिस प्रकार जीवनपर्यंत मनुष्य भोजन करता है उसी प्रकार)। प्राणी को सदा इन वस्तुओं को हृदय में बसाना होगा, तभी उसके मन से अज्ञान का अंधकार दूर होगा और ब्रह्मज्ञान का प्रकाश होगा।
गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी या किसी अन्य सिख गुरु की जीवनी अथवा सिख इतिहास का बखान नहीं है, बल्कि इसमें मात्र एक परम सत्ता की महिमा और व्यावहारिक जीवन-युक्ति का वर्णन है। इसमें वर्णन है ईश्वर के नाम-सिमरन का , प्रेमा-भक्ति का, जन सेवा का, जीवन में आडंबर व छल-कपट छोड़ने एवं नैतिक मूल्यों, पवित्रता और सादगी को अपनाने का। इसमें वर्णन है मानवीय एकता तथा भाईचारे का।
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब और राष्ट्रीय एकसूत्रता
राष्ट्रीय एकसूत्रता की बेजोड़ मिसाल है गुरु ग्रंथ साहिब। हालाँकि सिख धर्म का उदय पंजाब में हुआ और उसकी अधिकतर गतिविधियाँ भी पंजाब में ही केंद्रित रहीं, लेकिन गुरु अर्जुन ने गुरु ग्रंथ साहिब को ईश्वरीय वाणी का वह विशाल सागर बनाया जिसमें उत्तर- दक्षिण, पूर्व- पश्चिम चारों दिशाओं से ईश्वरस्तुति की सरिताएँ आकर समाहित हुई। उदाहरण के तौर पर, गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी वाणी के रूप में मौजूद संत नामदेव और संत परमानंद महाराष्ट्र के थे, तो संत त्रिलोचन गुजरात के। संत रामानंद दक्षिण में पैदा हुए तो संत जयदेव का जन्म पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से गाँव में हुआ। इसी प्रकार धन्ना का संबंध राजस्थान से था तो सदना सिंध से ताल्लुक रखते थे। इनकी तथा बाकी संतों- भक्तों की वाणी को एक माला में पिरोकर गुरु अर्जनदेव ने भारत के भौगोलिक समन्वय की बेहतरीन और अभूतपूर्व मिसाल कायम की।[3]
सिख गुरुओं ने अपनी वाणी, अपने संदेश और उपदेश से अँधेरे में भटकते लोगों को नई राह और नई रोशनी दिखाई। जीवन-रसायन से भरपूर गुरुओं की अमृत वाणी ने समाज को अकर्मण्यता, आडंबर, अंधविश्वास, अज्ञानता की अँधेरी सुरंग से बाहर निकालकर उसकी दशा और दिशा ही बदल दी। दस में से सात गुरुओं — पहले से पाँचवें, नौवें तथा दसवें गुरु ने वाणी की रचना की। ये वाणीकार गुरु हैं — गुरु नानक जी देव , गुरु अंगददेव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुनदेव, गुरु तेगबहादुर और गुरु गोबिंद सिंह। इनमें से सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह को छोड़कर शेष सभी छह वाणीकार गुरुओं की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। गुरु गोबिंद सिंह की वाणी अलग से ‘दशम ग्रंथ’ में संकलित है।
श्री गुरुनानक देव की समकालीन परिस्थिति और मुगल आक्रान्ताओं से त्रस्त भारत
दसवीं शताब्दी के साथ ही मध्य एशिया से मुसलमान आक्रान्ताओं के लगातार आक्रमण होने लगे। दिल्ली का मुख्य मार्ग पंजाब से गुज़रता था, इसलिए इसी प्रांत के लोगों को सबसे अधिक कष्ट भोगने पड़े। अफ़ग़ानों तथा तुर्क़ों ने अपने राज्य कायम किये, तथा विभिन्न मुस्लिम देशों ने उत्तरी भारत पर राज्य किया।
उस दौरान मुगलों का शासन था, इन मुस्लिम आक्रांताओं से समाज त्रस्त था। उस समय की भारत की सामाजिक और राजनीतिक जो दशा मुगलों के कारण थी उसका उल्लेख भी गुरु ग्रन्थ साहिब में मिलता है। जब गुरु नानक जी का जन्म हुआ, उत्तर भारत का शासक बहलोल लोदी था। उसके उत्तराधिकारी का नाम सिकन्दर लोदी था। इसके बाद इब्राहीम लोदी शासक बना। गुरु नानक जी के समय में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी, तथा बाद में उन्हीं के समय में बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायुँ उसका उत्तराधिकारी हुआ।
गुरु नानक ने अपनी रचना में इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि की है कि मुगलों और पठानों में युद्ध हुआ। उन्होंने (मुगलों ने) युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। पठानों ने अपने हाथियों को आगे बढ़ाया :
मुगल पठाणा भई लड़ाई रण महि तेग बगाई।
उन्हीं तुपक ताणि चलाई, उन्हीं हसति चिड़ाई।।
गुरु नानक ने अपने युग को केवल निरुपाय मूक दर्शक की भांति नहीं देखा था। उन्होंने समय के सम्पूर्ण त्रास और जन-जीवन की पीड़ा को अनुभव किया था, उसके प्रति अपनी करुणा, क्षुब्धता एवं आक्रोशयुक्त प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की थी और अन्याय अत्याचार के प्रति विरोध का संकेत भी किया था। गुरु नानक की यह दृष्टि उनके द्वारा प्रवर्तित मार्ग की अंतः प्रेरणा बनती है।[4]
विदेशी शासकों तथा उनके विदेशी प्रतिनिधियों ने सैन्यबल के आधार पर शासन किया। उन्होंने जनता का शोषण किया और अनगिनत अत्याचार किये, गैर-मुसलमानों पर जजिया नामक व्यक्तिगत टैक्स लगाया, यूं भी उन पर भारी कर लगाये। सिवाय छोटे पदों के बाकि सारे ऊँचे पदों पर हिन्दुओं की नियुक्ति के मार्ग बन्द थे। हिन्दू मंदिरों को ध्वस्त कर बड़ी संख्या में मस्जिदों का निर्माण हो रहा था। हिन्दू विद्यालयों को बन्द किया जा रहा था, और हिन्दू सभ्यता तथा संस्कृति को नष्ट’ करने का हर उपाय किया जा रहा था।
तलवार के ज़ोर पर बहुत-से हिन्दुओं को मुसलमान बनाया गया, तथा जनता के विश्वास को तोड़ा गया। शासकों और शासित के बीच खाई थी, तथा हिन्दू और मुसलमान आबादियों में भी भेद होता था, यहाँ तक कि हिन्दू संतों को सभी तरह के अपमान सहने पड़ते थे।
धर्मनिन्दा कानून को बड़ी सख्ती से लागू किया गया तथा इस्लाम की आलोचना के लिए प्राणदंड मिलता। बोधन ब्राह्मण को सिकंदर लोदी ने इसलिए प्राणदंड दिया कि उसने कहा था कि जैसा इस्लाम है वैसा ही हिन्दू धर्म भी है। हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तन हर समय होता रहता था, लेकिन विशेष अवसरों पर तथा देश के कुछ भागों में तो सामूहिक रुप से धर्म -परिवर्तन कराया जाता था ।
भाई गुरुदास जी की वारों में इस बात का संकेत मिलता है कि काजियों में रिश्वत का बोलबाला था। आदि श्री गुरुग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी के शब्दों में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है-
कलि होई कुते मुही खाजु होआ मुरदारु।
कूहु बोलि बोलि भउकणा चूका धरमु बीचारु॥
जिन जीवंदिआ पति नहीं मुइआ मंदी सोई।
लिखिआ होवै नानका करता सु होइ।
अर्थात् “कलियुग में (इस बुरे समय में) मनुष्य के मुख कुत्तों के समान हो गए हैं। धर्म के सम्बन्ध में मनुष्य के सारे विचार समाप्त हो गए हैं। जिनमें जीवित रहते हुए प्रतिष्ठा नहीं है, मरने के पश्चांत् उनकी अवश्य बुरी दशा होगी। जो कुछ भी भाग्य में लिखा होता है, वह अवश्य होता है। जो कर्ता (परमात्मा) करता है, वही होता है।
गुरु नानक देव ने तत्कालीन बादशाहों और उनके कर्मचारियों का चित्रण इस प्रकार किया है-
कलि काती, राजे कासाई धरमु पंखु करि उडरिआ ।
कूडु अमावस, सचु चंद्रमा दीसै नाही, कह चड़िया ॥
हउ भालि विकुंनी होई। आधेरै राहु न कोई ॥
विचि हउमै करि दुखु रोई। कहु नानक किनी बिधि गति होई ।।
(माझ, वार, महला-1)
अर्थात्, राजे कसाई के समान हो गए हैं, पुराना आदर्श कि राजा प्रजा का पिता होता है, समाप्त हो चुका है। रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। उनमें धर्म नाम का कोई तथ्य नहीं बचा है। वह तो जैसे पंख लगाकर उड़ गया हो। चारों ओर मिथ्या का प्रसार है, सत्य की ज्योति कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसी अव्यवस्था देखकर नानक व्याकुल हो रहे हैं। अधर्म के अँधेरे में मार्ग नहीं मिल रहा। समूची जनता अहंकार में फँसी पथभ्रष्ट हो रही है। गुरु नानक कहते हैं कि विदेशी शासकों के कारण भारतीयों की स्थिति दयनीय हो गई है। स्थिति यह हो गई है कि
आदि पुरख कउ अलहु कहिऐ सेखां आई वारी।
देवल देवतिआ करु लागा, ऐसी कीरति चाली।
कूजा बांग निवाज मुसला नील रूप बनवारी।
घरि घरि मीआ सभनां जीआं बोली अवर तुमारी।
जे तू मीर महीपति साहिबु कुदरति कउण हमारी।
चारे कुंट सलामु करहिगै धरि धरि सिफति तुम्हारी । (बसंत, अष्टपदी, महला-1)[5]
अर्थात् अब तो शेखों का ही बोलबाला हो गया है। इसलामी तुर्क शासकों के भय से आदिपुरुष परमात्मा को भी अल्लाह के नाम से ही बोलना पड़ रहा है। शासन ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि मंदिरों और देवताओं पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। भारतीयों को अपनी पूजा पद्धति का भी इस्लामीकरण करना पड़ रहा है। चारों ओर अजान की ही आवाज सुनाई पड़ रही है। हालत यहाँ तक हो गए हैं कि बनवारी यानी कृष्ण को भी नील वस्त्रधारी कहना पड़ रहा है। उनकों नील वस्त्रों में रखना पड़ रहा है। केवल इसलिए, ताकि विदेशी शासक प्रसन्न रहे। घर-घर ‘मियाँ-मियाँ’ शब्द गाया जा रहा है। लोगों की बोली ही बदल गई है। सब ओर सलाम-ही सलाम हो रहा है। सब लोग मुगलों की प्रशंसा में ही लगे हुए हैं। गुरु नानक देव कहते हैं कि इस कलियुग में विदेशी शासकों ने भारत में शरीअत को लागू कर रखा है। काजियों को ही अब कृष्ण बताया जा रहा है।[6]
इतिहास में बाबर के आक्रमण प्रसिद्ध हैं। सन् 1521 ई. में उसने अमीनाबाद पर आक्रमण किया और उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। स्त्रियों की दुर्दशा की गई। गुरु नानक देव ने इसका चित्रण अत्यधिक द्रवीभूत होकर किया है। उन्होंने अमीनाबाद के आक्रमण को स्वयं देखा था। वे उसका निम्नलिखित ढंग से वर्णन करते हैं-“जिन स्त्रियों की सुन्दर केश-राशि थी, जिनकी मांगे सिन्दूर से अनुरंजित रहा करती थीं, सिर के वे ही बाल कैंचियों से कतर दिए गए हैं और धूल उड़ उड़ कर गले तक आ रही है। जो सुन्दरियाँ महलों के भीतर निवास करती थीं, उन्हीं को आज साधारण स्थानों में बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है।………जो रमणियाँ गरी-छुहारे खाती थीं और पलँग पर आनन्द लेती थीं, उन्हीं के गले में रस्सियाँ पड़ी हुई हैं और उनकी मुक्ता-मालाएँ टूट टूट कर गिर रही हैं।
जिन सिरि सोहनि परीआ माँगी पाइ संधूरू।
से सिरि काती मुनीअन्हि गल विचि आवै धूढ़ि ॥
महला अंदर होरीआ हुणि बहणि न मिलन्ह हदूरि ॥
………..
गरी छुहारे खांदीआ माणन्हि सेजड़ीआ।
तिन्ह गल सिलका पाईआ। तुटन्हि मोतसरीआ ।।[7]
युद्ध के परिणामों पर भी गुरु नानक देव की पैनी दृष्टि गई है। उन्होंने कहा है-
कहां सु खेल तबेला घोड़े, कहां भेरी सहनाई ।
कहाँ सु तेगबन्द, गाडेरडि, कहा सु लाल कवाई ॥
कहां सु आरसीआ, मुंह बंके, ऐथै दिसहि नाही॥[8]
अर्थात् “तुम्हारे वे सब खेल कहाँ चले गए? तुम्हारे घोड़ों और अस्तबल का भी पता नहीं है। तुम्हारी तलवारों की म्यानें, तुम्हारे रथ, तुम्हारी लाल वर्दियाँ, तुम्हारे दर्पण, तुम्हारे सुन्दर मुख कहाँ विलीन हो गए ? वे यहाँ तो कहीं भी नहीं दिखायी पड़ रहे हैं!
गुरु नानक देव बाबर के आक्रमण और भारतवर्ष की दुर्दशा से अत्यन्त द्रवीभूत हुए। गुरु नानक जी इन क्रूरताओं के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना चाहते थे। उनका पवित्र, सरल, सच्चा और भावुक ह्रदय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक न सका। वे साहस, धैर्य, निर्भयता और दृढ़ता से परमात्मा से उसी भांति प्रश्न करते हैं, जिस भांति सरल बालक अपने पिता से उसके किसी रहस्यमय चरित्र का समाधान चाहता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं-
खुरासान खसमाना कीआ हिंदुस्तानु डराइआ ।
आपै दोसु न देई करता जमु करि मुगल चड़ाइआ ॥
एती मार पई करलाणे तै की दरदु न आइआ ॥१॥
करता तू सभंना का सोई ।
जे सकता सकते कड मारे ता मनि रोसु न होई ॥१॥ रहाड ॥
सकता सीहु मारे पै वगै खसमै सा पुरसाई ॥२॥[9]
अर्थात “बाबर ने खुरासान पर शासन किया, उसने हिन्दुस्तान को अपने आक्रमण से भयभीत किया। कर्ता (परमात्मा) ने अपने ऊपर दोष न रख कर मुगलों को यम रूप बना कर आक्रमण कराया। इतनी मारकाट हुईं और इतनी करुणा व्याप्त हुईं, पर हे परमात्मा क्या तुममें तनिक भी करुणा उत्पन्न नहीं हुईं ! हे. कर्ता, तू सभी का है (किसी वर्ग विशेष अथवा जाति विशेष का नहीं है) यदि कोई शक्तिशाली किसी शक्तिशाली का हनन करता है, तो मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होता। पर यदि शक्तिशाली सिंह निरपराध पशुओं के झुण्ड पर आक्रमण करता है, तो स्वामी को कुछ तो पुरुषार्थ दिखलाना चाहिए।
इस प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आए हुए गुरु नानक देव के पदों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतवर्ष की राजनीतिक अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी। पंजाब की दशा तो ओर भी चिन्तनीय थी। पहले पहल यही प्रान्त जीता गया था। उसकी स्थिति दो शक्तिशाली मुस्लिम राजधानियों–दिल्ली और काबुल के बीच में थी। वहाँ मुस्लिम साम्राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। गुरु नानक के पदों से स्पष्ट प्रत्तीत होता है कि वह समय रक्तपात का युग था। तलवारें सदा गर्दनों पर लटकी रहती थीं। आतंक का साम्राज्य सारे देश में व्याप्त था। कोई ऐसा नेता न था, जो राष्ट्र की समस्त बिखरी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर अत्याचार का सामना कर सके।
राजनीतिक धर्मान्धता का सामाजिक संघटन पर प्रभाव पड़ा। मुसलमान शासकों ने धर्म-परिवर्तन के कई अस्त्र निकाले, जिनमें यात्रा कर, तीथयात्रा कर, धार्मिक मेलों, उत्सवों और जुलूसों पर कठोर प्रतिबन्ध, नए मन्दिरों के निर्माण तथा जीर्ण-मन्दिरों के पुनरुद्धार पर रोक, हिन्दू-धर्म और समाज के नेताओं का दमन, मुसलमान होने पर बड़े बड़े पुरस्कार देने आदि मुख्य थे। इन्हीं अस्त्रों के द्वारा वे लोग हिन्दू-धर्म को सर्वथा मिटा देना चाहते थे।
इन अत्याचारों का परिणाम तत्कालीन जनता पर बहुत अधिक पड़ा। हिन्दुओं का अनुदार वर्ग ओर भी अधिक अनुदार बन गया। वे अपनी सामाजिक स्थिति के रक्षण के प्रति ओर भी अधिक सचेष्ट हो गए। इसका परिणाम हिन्दू-मात्र के लिए अत्यन्त भीषण सिद्ध हुआ। हिन्दुओं का एक वर्ग असहिष्णु, अनुदार और संकीर्ण हो गया। अपने को विधर्मी प्रभावों से बचाना उसका उद्देश्य हो गया। युग-धर्म, लोक धर्म से परामुख हो, बाह्यचारों, रूढ़ियों के कवच से अपने को सुरक्षित रखना, यही उनका सबसे बड़ा प्रयास सिद्ध हुआ। उनकी यह परामुखता अन्य धर्मावलम्बियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अपने सहधर्मियों के साथ भी व्यापक रूप में परिलक्षित हुईं। इसी कारण सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई।
भारतवर्ष में राजनीति और समाज का मेरुदण्ड धर्म ही रहा। यहाँ की राजनीतिक एवं सामाजिक-संघटन कभी धर्म-निरपेक्ष नहीं रहे हैं। गुरु नानक देव के समय में राजनीतिक एवं सामाजिक संकीर्णता एवं अत्याचारों और अनाचारों का मूल कारण धार्मिक संकीर्णता थी। उस काल के हिंन्दू एवं मुसलमान अपने अपने धर्म की उदार और सार्वभौमिक मान्यताओं को भूल कर साम्प्रदायिकता के गड्ढे में पड़े हुए थे। गुरु नानकदेव ने उसका सजीव चित्रण अपने शिष्य, भाई लालों से इस भाँति किया है—
सरमु धरसु दुइ छुपि खलोए कूडु फिरै परधानु वे लालो ।
काजीआ बामण की गलि थकी अगदु पड़े सैतानु वे लालो ॥
मुसलमानीआ पड़हि कतेबा कसट महि करहि खुदाइ वे लालो ।
जाति सनाती होरि हिंद्वाणीआ एहि भी लेख लाइ वे लालो ॥
खून के सोहिले गावीअहि नानक रतु का कंगू पाइ वे लालो ॥[10]
अर्थात्, “अरे लालो, लज्जा और धर्म–दोनों ही–संसार से विदा हो चुके हैं और चारों ओर झूठ का ही साम्राज्य हैं। काजियों और बाह्मणों ने अपने कर्तव्य त्याग दिए हैं और अब विवाह शैतान करवाता है। मुसलमान स्त्रियों और हिन्दू-स्त्रियों तथा समाज की अन्य स्त्रियाँ कष्ट में पड़ कर परमात्मा का नाम ले रही हैं। नानक कहते हैं कि वे सब खूनी गीत गा रही हैं और केसर के स्थान पर रक्त पड़ रहा है।
धर्म का वास्तविक रूप लोग भूले जा रहे थे। बाह्यडम्बरों का बोलबाला था। बहुत से लोग तो भय से और मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए कुरान इत्यादि पढ़ते थे। मुसलमान भी ‘असली मजहब’ को छोड़ रहे थे।
गुर नानक देव ने ‘आसा दी वार’ में कहा है “हिन्दू मस्तिष्क मुसलमानों की संस्कृति की इतनी दासता स्वीकार कर लिए है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुसलमानों को आत्म समर्पण कर दिए हैं।”[11] वास्तव में मुसलमानों के बलात धर्म-परिवत्तन एवं हिन्दुओं की मानसिक कमजोरी के कारण हिन्दुओं में बाह्यडम्बरों की प्रबलता आ गईं थी।
भाई गुरुदास जी ने अपनी वारों में तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति का इस प्रकार चित्रण किया है—“मुसलमानों में भी अनेक वेश चल पड़े हैं। कोई पीर है, तो कोई पैगम्बर और कोई औलिया। ठाकुरद्वारों को गिरा कर उनके स्थान में मस्जिदों का निर्माण किया गया है। गौ और गरीबों की हत्या करते हैं। इस भांति पृथ्वी के ऊपर पाप का विस्तार हो गया है।[12]
वस्तुतः उस समय की राजनीतिक स्थिति की भयंकरता, सामाजिक व्यवस्था की अस्त
[1] जगजीत सिंह, गुरु ग्रंथ साहब, पृष्ठ 31
[2] जगजीत सिंह, गुरु ग्रंथ साहब, पृष्ठ 32
[3] जगजीत सिंह, गुरु ग्रंथ साहब, पृष्ठ 35
[4] डॉ महीप सिंह,गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहब तक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 2005 पृष्ठ 4
[5] कुलदीप चंद अग्निहोत्री, लोकचेतना और आध्यात्मिक साधना के वाहक श्री गुरु नानक देव जी, प्रभात प्रकाशन, 2019, पृष्ठ 49
[6] कुलदीप चंद अग्निहोत्री, लोकचेतना और आध्यात्मिक साधना के वाहक श्री गुरु नानक देव जी, प्रभात प्रकाशन, 2019, पृष्ठ 50
[7] श्री गुरु ग्रंथ-दर्शन, जयराम मिश्र, साहित्य भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1960, पृष्ठ 41
[8] श्री गुरु ग्रंथ-दर्शन, जयराम मिश्र, साहित्य भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1960, पृष्ठ 41
[9] श्री गुरु ग्रंथ-दर्शन, जयराम मिश्र, साहित्य भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1960, पृष्ठ 42
[10] श्री गुरु ग्रंथ-दर्शन,जयराम मिश्र,साहित्य भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1960, पृष्ठ 47
[11] श्री गुरु ग्रंथ-दर्शन,जयराम मिश्र,साहित्य भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1960, पृष्ठ 48
[12] श्री गुरु ग्रंथ-दर्शन,जयराम मिश्र,साहित्य भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1960, पृष्ठ 49