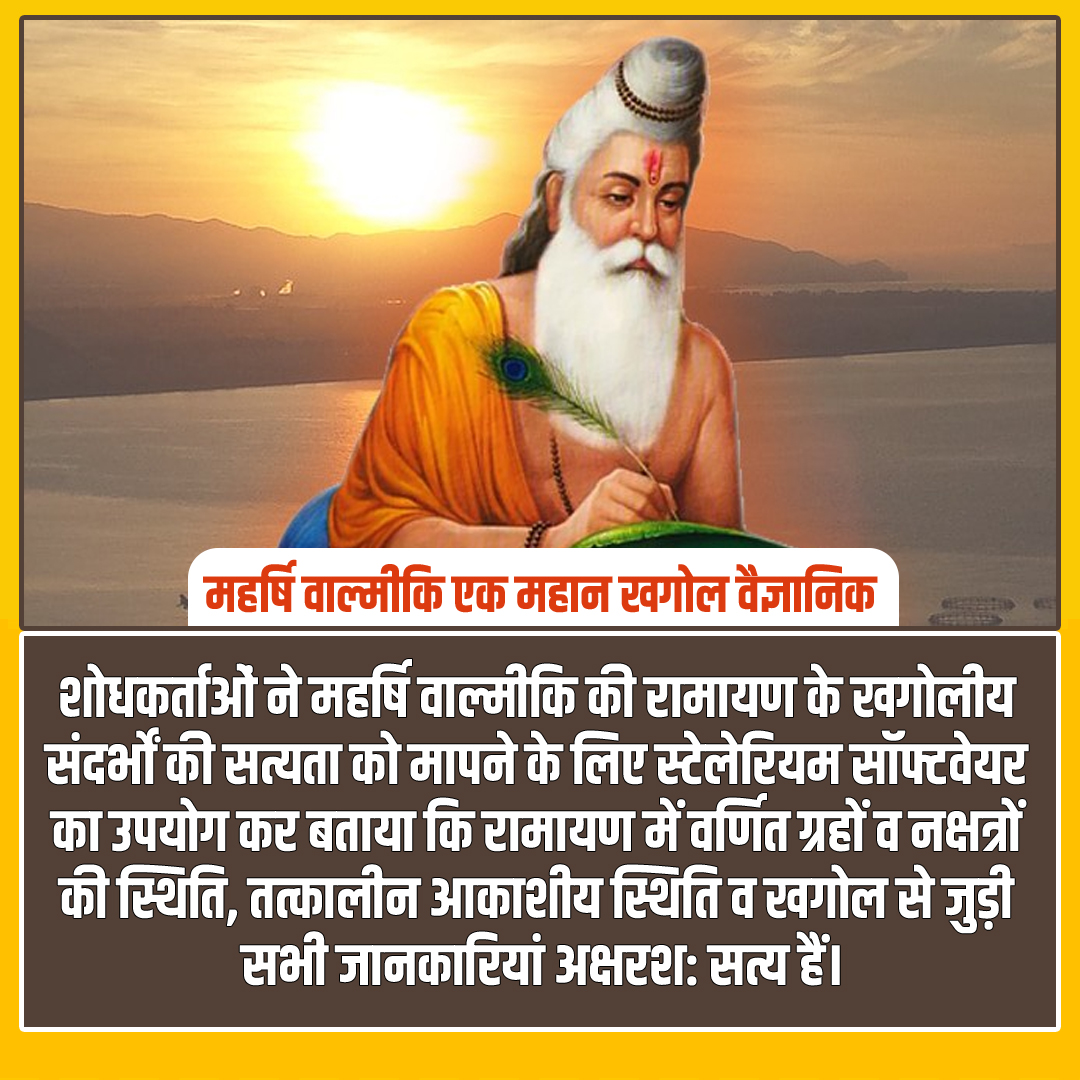आज शायद ही ऐसा कोई भारतीय मिले, जो महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य ‘रामायण’ से परिचित न हो। ‘रामायण’ मानवीय आदर्शो का मार्गदर्शक महाकाव्य है, इसीलिए उसे मानवीयता का पथ-प्रदर्शक आदर्श काव्य माना जाता है। सारे संसार में समादरणीय बने इस महाकाव्य के लिए हर भारतीय अभिमान का अनुभव करे तो कोई आश्चर्य नहीं। संसार भर में सबसे प्राचीन महाकाव्य ‘रामायण’ को आदिकाव्य होने का गौरव प्राप्त होना स्वाभाविक है। इसी कारण भगवान् श्री रामचंद्र के साधना चरित्र से जनता-जनार्दन परिचित हो सकी।
रामभक्ति के प्रचार-प्रसार के मूल में यही महाकाव्य समस्त विश्व में प्रतिष्ठित हुआ है। वाल्मीकि के रस महाकाव्य ने अनेक व्यक्तियों को रामभक्ति की प्रेरणा दी, जीवन को सार्थक बनाने का अवसर दिया। इसी आदिकाव्य से अभिभूत होकर अनेक कवियों ने भारत भर में प्रचलित अपनी-अपनी भाषाओं में रामकथापरक काव्य, महाकाव्य और नाटक लिखे। संत तुलसीदास का ‘रामचरितमानस’, संत एकनाथ का मराठी में लिखा ‘ भावार्थ रामायण’ या समर्थ रामदास का ‘युद्धकांड’- सबका आधार रामायण है। इस प्रकार के अन्यान्य काव्यों की भी एक लंबी परंपरा है।[1]
आदिकवि महर्षि वाल्मीकि
वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि को राम के समकालीन बताया गया है। आदिकवि वाल्मीकि एक श्रेष्ठ ऋषि, बुद्धिमान पंडित, लोक कल्याण के इच्छुक, तपस्वी, नीतिज्ञ, दयालु, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मज्ञ, भारतीय संस्कृति के रक्षक एवं आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि के व्यक्तित्व के विषय में विद्वानों के मत इस प्रकार हैं —
- महाकवि कालिदास ने ‘कृतवाग्द्वारे वंशऽस्मिन्-पूर्वसूरिभिः’ लिखकर वाल्मीकि को वाणी का द्वार खोलने वालों में अग्रगण्य अर्थात् आदि कवि एवं कवियों के मार्ग-दर्शक के रूप में माना है।[2]
- प्रसिद्ध काव्य शास्त्री आनन्दवर्धनाचार्य ने महषि वाल्मीकि को शोक एवं श्लोक का समीकरण करने वाला श्रेष्ठ समालोचक माना है।
- वाचस्पति गेरोला ने वाल्मीकि के विषय में लिखा है कि वे आदि कवि, महाकवि, धर्माचार्य और सामाजिक जीवन की बारीकियों के ज्ञाता सभी कुछ एक साथ थे, वे गम्भीर आलोचक भी थे।[3]
- डा० नानूराम व्यास ने लिखा है कि वाल्मीकि ऋषि समाज के अग्रगण्य तपस्वी, साधक, वेद वेदांगों के परिनिष्ठित विद्वान्, रस सिद्ध कवीश्वर, तत्कालीन भारत के मानचित्र के सम्यक ज्ञाता, सामाजिक प्रथाओं एवं मर्यादाओं के संस्थापक और व्याख्याकार सत्य और न्याय के समर्थक, धर्म के स्तम्भ एवं लोकानुरञ्जन के प्रबल हिमायती थे।[4]
- द्वितीय सरसंघचालाक गोलवलकर जी के अनुसार – “वाल्मीकि ने मानवीय विकास की चरम सीमा तक मानवी गुणों के अनुपम आदर के रूप में प्रभु रामचन्द्र को, मानवीय गुणों से युक्त एक मानव के रूप में ही प्रस्तुत किया। उनकी माता-पिता के प्रति भक्ति, भाइयों के प्रति स्नेह, पत्नी के प्रति प्रेम-उसकी करुणा और विशुद्धता में–सबके प्रेम का विषय बन गया है। ये और प्रतिदिन के मानव-जीवन के अन्यान्य पक्षों को इतने उत्कृप्ट रूप में रखा गया है कि जिनसे स्फूर्ति ग्रहण कर सर्वसाधारण मनुष्य अपने दैनिक जीवन को उस उज्जवल आदर्श के अनुसार ढाल सके तथा उन्नत कर सकें। जिन कठिनाइयों से वे पार निकले, माता-पिता तथा बाद मे अर्धांगिनी के विंयोग का दुख सहन किया और अंत में पाप एवं अधर्म की शक्तियों पर उन्होंने जो विजय प्राप्त की, उससे हमारे हृदय में आशा की लहर पंदा होती है, विश्वास का अंकुर उगत्ता है। अदम्य साहस की स्फूर्ति प्राप्त होती है और समस्त आपत्तियों से लोहा लेकर, उन पर विजय प्राप्त कर इस पृथ्वी पर अपने को ईश्वरीय प्रतिमा के अनुरूप हम बना सकते है।“ [5]
- श्री दत्तोपंत ठेंगडी के अनुसार – “वाल्मीकि रामायण का प्रभाव भारतवासियों के जीवन पर, आचारों पर, विचारों पर, कर्मों पर, व्रतों पर, नियमों पर तथा कल्पनाओं तक पर बहुत गहरा अंकित हुआ दिखाई देता है। भारतीय हृदय में पितृ-पूजन के, वधु-भावना के, यति या सती धर्म के, तप-त्याग के, लोकसेवा के, समाज-संगठन के, लोकसंग्रह के, जाति या देश हित के, न्याय तथा सर्वोत्तम शासन के आदर्श श्रीराम ही माने जाते है। हमारे लिए धार्मिक दृष्टि से भी शुभ कर्मो के लिए परम पावत प्रतीक वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामचन्द्र है।“[6]
वस्तुतः भारतीय संस्कृति एवं धर्म के रक्षक के रूप में अपनी कृति के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि आज भी प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व की प्रतिमा बन कर हमारे समक्ष उपस्थित है।
आदिकाव्य ‘रामायण’
- रामायण संस्कृत भाषा के काव्यों में सबसे प्रथम रचना मानी जाती है अतः यह आदि काव्य भी है। वाल्मीकि रामायण में भी इस काव्य को आदिकाव्य कहा गया है।
- रामायण आदि काव्य है इसकी पुष्टि वाल्मीकि के बाद के कवियों ने भी की है। महाकवि कालिदास ने रामायण को ‘पहली कविता’ के रूप में स्वीकार किया है।” करूण रस के कवि भवभूति ने रामायण को आदि काव्य स्वीकार करते हुये ‘मा निषाद प्रतिष्ठा पद’ को लक्ष्य करके उत्तर रामचरित में लिखा है कि वेद से अन्यत्र भी छन्द का नया आविर्भाव हो गया। भवभूति ने वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा दी है। आनन्दवर्धन ने अपनी कृति में वाल्मीकि को आदि कवि कहा है।
- सभी विद्वानों ने भी वाल्मीकि को आदिकवि और उनकी कृति रामायण को आदिकाव्य माना है। डा० रामस्वामी इस विषय में लिखते है कि वाल्मीकि निःसंदेह आदि कवि हैं, वे प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम कवि है। सवसम्मति से वाल्मीकि आदिकवि ओर उनकी कृति रामायण आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है।
रामायण में सात खण्ड हैं। वे इस प्रकार है– बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड, एवं उत्तरकाण्ड। इस कृति में २४००० श्लोक, ५०० सगर एवं १०० उपाख्यान है।
रामायण का नामकरण — रामायण पद रामस्य अयनम से निर्मित है। रामायण का अर्थ राम का मार्ग या राम के जीवन मार्ग को प्रकाशित करने वाला काव्य रामायण है।
वाल्मीकिकृत रामायण के तीन पाठ
वाल्मीकिकृत रामायण का पाठ एकरूप नहीं है। आजकल इस रचना के तीन पाठ प्रचलित हैं :
(1) दाक्षिणात्य पाठ: गुजराती प्रिंटिंग प्रेस (बम्बई), निर्णय सागर प्रेस (बम्बई) तथा दक्षिण के संस्करण। यह पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित और व्यापक है।
(2) गौडीय पाठ : गोरेसियो (पैरिस) तथा कलकत्ता संस्कृत सिरीज के संस्करण|
(3) पश्चिमोत्तरीय पाठ: दयानन्द महाविद्यालय (लाहौर) का संस्करण, जो आजकल साधु आश्रम, होशिआरपुर (पंजाब) से प्राप्त है|
प्रत्येक पाठ में बहुत से श्लोक ऐसे मिलते हैं जो अन्य पाठों में नहीं पाये जाते। दाक्षिणात्य तथा गौडीय पाठों की तुलना करने पर देखा जाता है कि प्रत्येक पाठ में श्लोकों की एक-तिहाई संख्या केवल एक ही पाठ में मिलती है। इसके अतिरिक्त जो श्लोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं उनका पाठ भी एक नहीं है और इनका क्रम भी बहुत स्थलों पर भिन्न है|[7]
इन पाठान्तरों का कारण यह है कि वाल्मीकिकृत रामायण प्रारंभ में मौखिक रूप से प्रचलित थी और बहुत काल के बाद भिन्न-भिन्न परम्पराओं के आधार पर स्थायी लिखित रूप धारण कर सकी। फिर भी कथानक के दृष्टिकोणों से तीनों पाठों की तुलना करने पर सिद्ध होता है कि कथावस्तु में जो अंतर पाए जाते हैं वे गौण हैं।
महर्षि वाल्मीकि की ‘रामायण’ का विश्वव्यापी प्रभाव
द्वितीय सरसंघचालाक गोलवलकर जी के अनुसार– “भारतवर्ष के लोगो के सम्मुख प्रभु रामचन्द्र का जीवन एक आदर्श पुरुष, मानव-सामर्थ्य के लिए जो सर्वोत्तम उन्नति सम्भव हो सकती है, उसे मर्यादा पुरुषोतम के रूप में अंकित किया गया है। रामचरित्र के महान् गायक वाल्मीकि ने प्रभु रामचन्द्र के अवतार पर विश्वास होते हुए भी बहुत प्रयत्नपूर्वक उनको अद्भुत, रहस्यमय एवं दैवी शक्तियों से युक्त अवतार के रूप में चित्रित नहीं किया है, अपितु मानवीय गुणो, मानवीय भावनाओं तथा मानवीय सामर्थ्य-सम्पन्न एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है।[8]
विश्व के अलग-अलग देशों में राम की अलग-अलग कथाएं प्रचलित हैं। कहीं पर राम की कथा मौरीसस की राम कथा का रूप ले लेती है तो कहीं पर किसी अन्य देश की राम कथा के रूप में वह अपना महत्त्व बनाए हुए है। ए. के. रामानुजन के अनुसार- “रामायणों की संख्या और पिछले पच्चीस सौ या उससे भी अधिक सालों से दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में उनके प्रभाव का दायरा हैरतनाक है। जितनी भाषाओँ में रामकथा पायी जाती है, उनकी फेहरिस्त बताने में ही आप थक जाएंगे : अन्नामी, बाली, बंगाली, कम्बोडियाई, चीनी, गुजराती, जावाई, कन्नड़, कश्मीरी, खोटानी, लाओसी, मलेशियाई, मराठी, ओडिया, संस्कृत, प्राकृत, संथाली, सिंहली, तमिल, तेलुगु, थाई, तिब्बती- पश्चिमी भाषाओँ को छोड़कर यह हाल है”।[9]
वस्तुतः रामकथा के अलग-अलग अनुवाद होते गए और कालांतर में अनेक देशों में वहाँ की संस्कृति और परिवेश के अनुकूल रामकथा अपना रूपाकार लेती गई और वहाँ के लोक जीवन में रच बस गई।
सन्दर्भ ग्रन्थ
- दाजी पणशीकर, रामायण के 51 प्रेरक प्रसंग, ग्रन्थ अकादमी, नई दिल्ली
- विश्वनाथ लिमये, वाल्मीकि के ऐतिहासिक राम, सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली
- दे. एच. याकोबी, दस रामायण
- वाल्मीकि रामायण हिंदी, राजपाल प्रकाशन
- ए. के. रामानुजन, तीन सौ रामायणे
- फ़ादर कामिल बुल्के, रामकथा: उत्पत्ति और विकास, हिंदी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित
- इलपावुलूरि पाण्डुरंगराव, भारतीय साहित्य के निर्माता वाल्मीकि, साहित्य अकादेमी, दिल्ली
[1] दाजी पणशीकर, रामायण के 51 प्रेरक प्रसंग, ग्रन्थ अकादमी, नई दिल्ली
[2] रघुवंशमहाकाव्यं, प्रथम सर्ग, श्लोक 4
[3] संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 202
[4] रामायण कालीन समाज, पृष्ठ 6
[5] विश्वनाथ लिमये, वाल्मीकि के ऐतिहासिक राम, स्वगत कथन से उद्धृत, सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली
[6] विश्वनाथ लिमये, वाल्मीकि के ऐतिहासिक राम, पुस्तक की प्रस्तावना से उद्धृत, सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली
[7] दे. एच. याकोबी, दस रामायण, पृष्ठ 3
[8] विश्वनाथ लिमये, वाल्मीकि के ऐतिहासिक राम, स्वगत कथन से उद्धृत, सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली
[9] ए. के. रामानुजन, तीन सौ रामायणे