रवीन्द्रनाथ ठाकुर : “मैंने संसार के विभिन्न भागों की यात्रा की है। इस यात्रा में मुझे अनेक संत और ऋषियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परन्तु, यह सत्य है कि मुझें कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं मिला जो केरल के श्री नारायण गुरु से महान हो। और न ही कोई ऐसा व्यक्तित्व मुझे ऐसा मिला है जिसने इनके समान आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की हो। मुझे विश्वास है कि मैं उस तेजस्वी व्यक्तित्व को कभी नहीं मूल सकता जो देवी आलोक के स्वप्रकाश से दैदीप्यमान हो। मैं उन योगी नेत्रों को भी नहीं भूल सकता जो दूर क्षितिज में स्थिर अनिर्मेष भाव से स्थिर थीं।“[1]
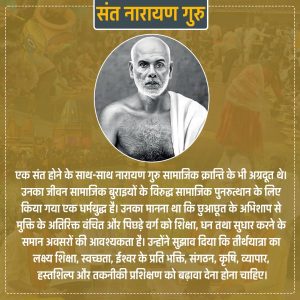
रोमां रोलां : “श्री नारायण गुरु की शिक्षा शंकराचार्य के दर्शन से प्रभावित है। वे वास्तविक अर्थ में कर्मज्ञानी एवं धर्मवेत्ता थे।…गाँधी, नारायण गुरु को सदैव पुण्यात्मा श्री नारायण गुरु कहा करते थे। वह हरिजन उत्थान के कार्यो में गुरु के विचारों को अपनाया करते थे। आज के विश्व में, और विशेषकर भारत के संदर्भ में, श्री नारायण गुरु का जीवन, उनके संदेश एवं उनके क़ृतित्व अपना विशेष महत्त्व रखते हैं।“[2]
आध्यात्मिक क्रांति के अग्रदूत
श्रीनारायण गुरु एक ऐसे युगांतकारी व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने दार्शनिक विचारों से समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, वे शंकर वेदांत के अनुयायी हैं, लेकिन उनके दार्शनिक विचारों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मनुष्य और समाज के संदर्भ में उन्होंने जब अद्वैत वेदांत का अनुप्रयोग किया, तो उसमें आमूल परिवर्तन किया और अद्वैत सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत कीं।
श्रीनारायण गुरु वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने एक पददलित समाज को फिर से मानव बनाने के लिए अद्वैत वेदांत का सहारा लिया। श्रीनारायण गुरु ने सूत्र वाक्य दिया कि “एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर मनुष्य का।“ अद्वैत के आधार पर उन्होंने मानव का एकत्व और मानव समाज की एकता पर बल दिया। अद्वैत के आधार पर एक नए विश्व का निर्माण ही उनका लक्ष्य था।
वर्ष 1888 की शिवरात्रि के दिन श्री नारायण स्वामी ने ऐतिहासिक शिवलिंग-प्रतिष्ठा का कार्य किया। अस्पृश्य जाति के एक अब्राह्मण द्वारा शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना केरल के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। इस दिन मंदिर की दीवार पर उन्होंने जो वाक्य अंकित किया था, वह एक नई आध्यात्मिक क्रांति का उद्घोष था। वह वाक्य एक काव्यांश के रूप में था :
“जाति भेदं, मत द्वेष एतुमिल्लाते सर्वंरु,
सोदरत्वेन वाषुन्न, मातृका स्थानमाणितु”
(जाति भेद, धर्म विद्वेष इन सबके बिना सभी जहाँ भाईचारे से रहते हैं, वह आदर्श स्थान है यह।)
वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण के द्वारा भारत की महान आध्यात्मिक संस्कृति और विश्वबन्धुत्त्व का उद्घोष किया। लेकिन उससे पाँच साल पहले ही 1888 में आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित जनसमूह के लिए नया शिव मंदिर बनाकर श्री नारायण गुरु ने उसमें लिखा कि यहाँ पर प्रवेश के लिए जातिभेद और धर्म का भेद कोई बंधन नहीं है। सभी जातियों और सभी धर्मों के लिए यह आध्यात्मिक केंद्र खुला है। भारतीय संस्कृति के सार्वजनीन, उदार आध्यात्मिक स्वरूप का यह उद्घोष था। धर्मों से परे जो आध्यात्मिकता है और अद्वैत का जो परम तत्त्व है, उसका प्रतिपादन श्रीनारायण गुरु ने किया। यह एक संयोग है कि 1893 के बाद के अपने भाषणों में इन्हीं तत्त्वों की व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में की थी। इस दृष्टि से एक नई आध्यात्मिक क्रांति के रूप में श्रीनारायण गुरु का ऐतिहासिक प्रदेय है।[3]
दलितों के उद्धार में सक्रिय योगदान
श्रीनारायण गुरु के समय केरल में ईषव जनजाति को अस्पृश्य माना जाता था, उनसे भी नीचे अनेक जातियाँ थी, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जातियाँ या दलित जातियाँ माना गया। श्रीनारायण गुरु सभी दलित जातियों का उत्थान चाहते थे और उन्होंने अपने द्वारा स्थापित मंदिरों में सभी दलित लोगों को प्रवेश दिया था। उनके द्वारा स्थापित तलश्शेरी के जगन्नाथ क्षेत्र आदि में दलितों के प्रवेश पर पहले कुछ तिय्य लोग आपत्ति कर रहे थे, लेकिन गुरु के प्रभाव से बाद में सभी जातियों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई। गुरु ने शिवगिरि और आलुवा में जो पाठशालाएँ शुरू कीं वहाँ पुलय आदि कई दलित जातियों के बच्चों को प्रवेश दिया।1907 में ‘श्रीनारायण धर्म परिपालन योगं’ की तरह ‘साधु जन परिपालन संघं’ नामक संगठन बनाकर दलितों के उद्धार के लिए काम करना शुरू किया।[4]
स्वामी ने बरकल और आलवै की संस्थाओं आदि में दलित वर्गों को प्रवेश दिया। अनेक ऐजावा जनजाति के नेताओं ने इसका अनुसरण करते हुए अपने घर में नौकर और रसोइये के रूप में दलित जाति के लड़कों को रखा। इस प्रथा का अर्थ इस बात से ठीक तरह से समझा जा सकता है कि तत्कालीन भारत में नौकर शीघ्र ही घर का सदस्य बन जाता था। हममें से वे भारतीय जो चालीस वर्ष से ऊपर के हैं, उन्हें अब भी याद होगा कि घर का नौकर किस प्रकार हमें मामा की तरह हमारी गलतियों के लिए दंड देता था। इस प्रकार जब निम्न जाति के लोग घर की परिधि में सम्मिलित होने लगे तो जातियाँ एक-दूसरे के निकट आयीं।[5]
ऐजावा जो संख्या में लाखों थे थिय्यास, चौवान, थानदान आदि उपजातियों में बंटे हुए थे और ये अन्तर्जातीय विवाह नहीं करते थे। स्वामी जी के आगमन से समूचे केरल में ये सब उपजातियाँ एक समुदाय में ढल गयी। ऐजवाओं के मन्दिर, शिक्षा संस्थाएं, छात्रावास आदि सभी जातियों के लिए खोल दिए गये। ऐजावाओं की बहुत सी उपजातियाँ अब तक अलग-अलग और छोटे छोटे वर्गों में रह रही थीं। उन सबको मिलाकर जब एक बड़ा समुदाय बना दिया गया तो नायर एवं अन्य जातियों ने भी अपने उत्थान के लिए ऐसा ही किया। साथ ही, श्री नारायण गुरु की इन गतिविधियों से इतना प्रभाव पड़ा कि केरल की सभी जातियों की आँखें खुल गईं और उन्होंने अपने अपने रीति-रिवाजों में सुधार लाने के लिए काम किया। अब तक अर्थात् बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामाकृष्ण मिशन एवं भारत समाज सेवक आदि के समाज-सुधार आन्दोलन और गतिविधियों का केरल समाज पर काफी प्रभाव पड़ा।[6]
श्री नारायण गुरु ने अपनी विनीत पद्धति से रूढ़िवादिता को जड़ से उखाड़ने का जो बीज बोया था उससे पचास वर्ष की छोटी अवधि में ही अच्छे परिणाम निकले। अछूतोद्धार के बारे में केरल में जितनी अभूतपूर्व प्रगति हुई उतनी भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं हुई।
मद्य-वर्जन : 1921 में ही उन्होंने कहा था–“शराब जहर है। इसका न तो उत्पादन किया जाना चाहिए और न इसे बेचना चाहिए और न ही पीना चाहिए।”[7]
श्री नारायण धर्म परिपालन योगम्
1903 में गुरु की छत्रछाया में श्री नारायण धर्म परिचालन योगम् नामक सभा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य श्री नारायण के विचारों का आम जनता में प्रचार तथा केरल के दलित वर्ग का उत्थान था। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता था।[8]
आलुवा का सर्वधर्म सम्मेलन
1924 में श्री नारायण गुरु ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को आलुवा अद्वैत आश्रम में एक सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया। भारत के सभी प्रदेशों से प्रतिनिधि उसमें भाग लें, इसकी व्यवस्था करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। अगर भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी अपने-अपने धर्मों की बुनियादी बातें एक ही मंच पर प्रकट करें तो धर्मों के बीच की बुनियादी एकता को सब लोग समझ सकते हैं, ऐसा उनका कथन था। भिन्नताएं और परस्पर विरोधी तत्त्व केवल बाहरी हैं, उनके आधार पर तर्क-वितर्क करना और आपस में झगड़ा करना व्यर्थ है। सभी धर्मों को आपस में मिलानेवाले सारभूत तत्वों का अवगाहन करना ही प्रमुख बात है। सभी दृष्टियों से 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन की तरह 1924 में आलुवा में सम्पन्न हुआ सर्वधर्म सम्मेलन भी ऐतिहासिक महत्त्व का सिद्ध होता है।[9]
मंदिरों के निर्माण में अहम् योगदान
श्रीनारायण गुरु ने लोगों के आग्रह पर मंदिरों का निर्माण किया बाद में उन्होंने स्वयं की इच्छा से कई आश्रमों का निर्माण भी किया। श्रीनारायण गुरु ने उन तथाकथित आधुनिकतावादी व्यक्तियों की इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मंदिर की यह इमारत शीघ्र ही बेकार हो जाएगी।
श्री नारायण गुरु ने कहा, “ऐसा कैसे सम्भव है? मंदिरों को साफ-सुथरा रखना चाहिए। लोग वहाँ आयेंगे, स्नान करेंगे और ताजगी का अनुभव करेंगे, साफ-सुथरे कपड़े पहनेंगे। इस प्रकार पूजा के लिए इकठ्ठे हुए लोगों के मन में सदविचार पैदा होंगे। उनकी बातचीत शीघ्र ही उत्तम विचारों में बदल जायेगी। वे स्वच्छ हवा का सेवन करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। इनमें से कुछ पूजा करेंगे और कुछ व्रत रखेंगे। इस सबसे वे पायेंगे कि उनकी सांसारिक चिन्ताओं का शमन हो रहा है और उन्हें मानसिक शान्ति मिल रही है। यही विश्वास दूसरों में भी (मन्दिरों के प्रति) आकर्षण पैदा करेगा। सभी कुछ तो विश्वास पर निर्भर है। क्या ये सब इसके लाभ नहीं है? अत: मंदिर तो आवश्यक है। हाँ उनका दुरुपयोग न कीजिए तभी आप उनकी उपयोगिता का पता लगा पायेंगे।[10]
गुरु जी ने विभिन्न अवसरों पर यहाँ तक सुझाव दिए थे कि इन मंदिरों का स्कूलों, पुस्तकालयों, सभा-कक्षों और सूत कातने के लिए स्थलों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
| नैरेटिव | काउंटर तथ्य |
| क्या श्री नारायण गुरु सनातन धर्म के अनुयायी नहीं थे ? | श्री नारायण गुरु शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से प्रभावित थे और उन्होंने विभिन्न स्थानों पर मंदिरों की स्थापना की जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तित्त्व ही थे :-
1. उन्होंने अरविपुरम में शिवमंदिर की प्रतिष्ठा की और इसके पश्चात वैकोम के चिरायनकिजू नामक स्थल पर देवश्व्रम मंदिर की स्थापना की। 2. 1893 में उन्होंने त्रिवेन्द्रम के उत्तर में कुलाथुर में प्राचीन भगवती मन्दिर के स्थान पर शिव की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध कौवलम् के निकट ही कुन्नुमपारा मन्दिर की स्थापना की। यह मन्दिर महत्वपूर्ण मन्दिरों में अपना स्थान रखता है। यह मन्दिर एक प्रपाती शिला पर बना हुआ है और इसका निर्माण अनगढ़ पत्थरों से बहुत ही सुन्दर ढंग से हुआ है। वास्तव में गुरू, श्री नारायण मन्दिरों के लिए प्राय: उन्हीं स्थलों का चयन करते थे जो अलौकिक सौन्दर्य से परिपूर्ण हों। इसीलिए और इसी प्रकार उन्होंने केरल के अत्यन्त सम्मोहक स्थल वरकला को अपने धार्मिक मुख्यालय के लिए चुना था। 3. 1904 में जब गुरु जी वरकला में आये तो उसकी पूर्वी पहाड़ी के अभूतपूर्व सौन्दर्य ने उन्हें इतना मोहित किया कि उन्होंने वहाँ एक छोटी-सी पर्णशाला बनायी और शाक-वाटिका लगायी। 4. 1912 में वैदिक विद्यालय के साथ-साथ एक सरस्वती मंदिर की भी स्थापना भी की। 5. अद्वैत आश्रम : गुरु जी ने अलवे में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। इस भवन का स्थान भी बहुत आकषंक है। अतः यह स्पष्ट होता है कि श्री नारायण गुरु ने मंदिरों का विकास किया जोकि उनके सच्चे सनातन धर्मी होने का परिचायक है। श्री नारायण गुरु के जीवन एवं आचरण से यह स्पष्ट है कि वे शुद्ध एवं सहज वेदान्ती थे। |
[1] श्री नारायण गुरू, मुर्कोट कुन्नहप्पा (अनुवादक डॉ. धर्मपाल गाँधी), नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 1985, आमुख से उद्धृत
[2] श्री नारायण गुरू, मुर्कोट कुन्नहप्पा (अनुवादक डॉ. धर्मपाल गाँधी), नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 1985, आमुख से उद्धृत
[3] श्रीनारायण गुरु : आध्यात्मिक क्रांति के अग्रदूत, प्रो. जी. गोपीनाथन, ज्ञान गंगा, दिल्ली, 2024, पृष्ठ 30
[4] श्रीनारायण गुरु : आध्यात्मिक क्रांति के अग्रदूत, प्रो. जी. गोपीनाथन, ज्ञान गंगा, दिल्ली, 2024, पृष्ठ 83
[5] श्री नारायण गुरू, मुर्कोट कुन्नहप्पा (अनुवादक डॉ. धर्मपाल गाँधी), नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 1985, पृष्ठ 49
[6] श्री नारायण गुरू, मुर्कोट कुन्नहप्पा (अनुवादक डॉ. धर्मपाल गाँधी), नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 1985, पृष्ठ 50
[7] श्री नारायण गुरू, मुर्कोट कुन्नहप्पा (अनुवादक डॉ. धर्मपाल गाँधी), नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 1985, पृष्ठ 64
[8] श्री नारायण गुरू, मुर्कोट कुन्नहप्पा (अनुवादक डॉ. धर्मपाल गाँधी), नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 1985, पृष्ठ 51
[9] श्रीनारायण गुरु : आध्यात्मिक क्रांति के अग्रदूत, प्रो. जी. गोपीनाथन, ज्ञान गंगा, दिल्ली, 2024, पृष्ठ 105
[10] श्री नारायण गुरू, मुर्कोट कुन्नहप्पा (अनुवादक डॉ. धर्मपाल गाँधी), नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 1985, पृष्ठ 30
