बौद्धिकों का एक प्रभावशाली समूह, जो मानता है कि भारत का अस्तित्व 15 अगस्त को हुआ था, हमेशा स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका पर सवाल उठाता है। वे इतिहास को छिपाने और यह तस्वीर पेश करने में अधिक रुचि रखते हैं कि आरएसएस कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं था। बौद्धिक यह तर्क देने के आदी हो चुके हैं कि स्वतंत्रता महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम थी।
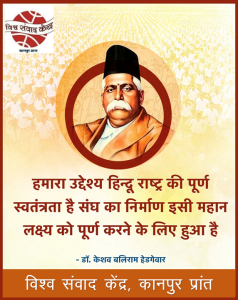
इस प्रक्रिया में, वे लाल, बाल और पाल की जानबूझकर उपेक्षा करते हैं। वे क्रांतिकारियों द्वारा किए गए कार्य की उपेक्षा करते हैं। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए महान प्रयासों को पहचानना आवश्यक नहीं समझते। इस प्रक्रिया में, ये बुद्धिजीवी उन सभी के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया और स्वतंत्रता के लिए अपनी सारी ऊर्जा समर्पित कर दी। आरएसएस के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने 1921 और 1930 में दो सत्याग्रह में भाग लिया था। दोनों ही मौकों पर उन्हें जेल हुई थी।
‘भारत छोड़ो’ आंदोलन शुरू होने से पहले 1940 में उनका निधन हो गया था। इस बात को उजागर करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को यह विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाता है कि स्वतंत्रता लाने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र जरिया थी। ऐसा आभास कराया जाता है कि भारत ने 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के कारण स्वतंत्रता हासिल की, जिसे महात्मा गांधी और कांग्रेस ने शुरू किया था।
लेकिन यह आधा सच है।
निःसंदेह, सत्याग्रह, चरखा और खादी सामान्य लोगों से जुड़ने के सरल साधन थे, लेकिन उन लाखों लोगों के योगदान की उपेक्षा करना, जिन्होंने अपने-अपने तरीकों से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, एक घोर अन्याय है। वास्तव में, यह उनके देशभक्तिपूर्ण कार्यों का अपमान है।
डॉ. हेडगेवार और स्वतंत्रता आंदोलन
आरएसएस के संस्थापक डॉ. हेडगेवार के मामले को लीजिए। उनका जन्म 1889 में नागपुर में हुआ था। नागपुर में स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा 1904-1905 में शुरू हुई। 1904-1905 से पहले नागपुर में स्वतंत्रता आंदोलन के शायद ही कोई लक्षण दिखाई दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि 1897 में डॉ. हेडगेवार से जुड़ी एक घटना हुई, जो डॉ. हेडगेवार के जन्मजात रवैये को दर्शाती है। याद रखें – जब यह घटना हुई तब डॉ. हेडगेवार केवल आठ साल के थे।
1897 में, महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के हीरक जयंती उत्सव को मनाने के लिए छात्रों के बीच मिठाइयां वितरित की गईं। हालांकि, आठ साल के लड़के ने मिठाई लेने से इनकार कर दिया। वास्तव में, उसने मिठाइयों को कूड़ेदान में फेंक दिया। यह कार्य देशभक्ति की भावनाओं और गुलामी के खिलाफ गुस्से की अभिव्यक्ति से कम नहीं था।
1907 में, रिसले सर्कुलर द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का जाप करना प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, केशव ने अपने नील सिटी स्कूल में सरकारी इंस्पेक्टर के सामने कक्षा में वंदे मातरम का जाप किया। परिणामस्वरूप, स्कूल प्रशासन ने इस कृत्य के लिए केशव को निष्कासित कर दिया।
यह घटना भी डॉ. हेडगेवार की देशभक्ति की भावनाओं को दर्शाती है।
स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद, डॉ. हेडगेवार ने मेडिकल की पढ़ाई में दाखिला लिया। डॉ. हेडगेवार के लिए मुंबई जाना स्वाभाविक होता, जहां मेडिकल शिक्षा की बेहतर सुविधाएं थीं। हालांकि, डॉ. हेडगेवार ने कलकत्ता जाना पसंद किया। डॉ. हेडगेवार ने कलकत्ता जाना चुना क्योंकि वह क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था। डॉ. हेडगेवार जल्द ही क्रांतिकारियों के शीर्ष निकाय अनुशीलन समिति में शामिल हो गए।
मेडिकल की शिक्षा पूरी करने के बाद, केशव 1916 में नागपुर लौट आए। उस समय शिक्षित लोगों के लिए शादी करना, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना और स्वतंत्रता आंदोलन सहित अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना एक सामान्य चलन था। सामान्य परिस्थितियों में डॉ. हेडगेवार भी यही रास्ता चुनते। हालांकि, न तो उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की और न ही शादी की। डॉ. हेडगेवार ने अपनी पूरी क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने कभी अपने निजी जीवन के बारे में नहीं सोचा।
डॉ. हेडगेवार लोकमान्य तिलक के कट्टर अनुयायी थे। 1920 में, कांग्रेस ने नागपुर में अपना अधिवेशन आयोजित किया, जब डॉ. हेडगेवार, डॉ. हार्डीकर के साथ, सभी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती की थी। उस समय डॉ. हेडगेवार नागपुर कांग्रेस के संयुक्त सचिव थे।
कांग्रेस अधिवेशन में एक उल्लेखनीय घटना हुई। डॉ. हेडगेवार ने एक प्रस्ताव का सुझाव दिया कि कांग्रेस को भारतीय गणराज्य की स्थापना का लक्ष्य रखना चाहिए, जो पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त होगा।
उन्होंने प्रस्ताव समिति के समक्ष पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिया। हालांकि, उनके प्रस्ताव को प्रस्ताव समिति ने नजरअंदाज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि नौ साल बाद लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने यही प्रस्ताव अपनाया। लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव के कारण डॉ. हेडगेवार बहुत खुश हुए और उन्होंने सभी आरएसएस शाखाओं को बधाई संदेश भेजा। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी।
लोकमान्य तिलक के निधन के बाद, महात्मा गांधी ने कांग्रेस नेतृत्व संभाला। महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। उसी अवधि के दौरान, अंग्रेजों ने तुर्किस्तान में खिलाफत को समाप्त कर दिया, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों को ठेस पहुंची। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हालांकि, महात्मा गांधी के इस रुख का कई कांग्रेस नेताओं और राष्ट्रवादी मुसलमानों ने स्वागत नहीं किया।
इस कारण नागपुर में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने कभी गति नहीं पकड़ी। अलग राय होने के बावजूद, डॉ. हेडगेवार, डॉ. चोलकर और शमीमुल्ला खान आदि ने इस स्थिति को बदल दिया। उनमें से किसी ने भी राष्ट्रीय हित में खिलाफत आंदोलन पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति नहीं जताई। डॉ. हेडगेवार ने पूरे मन से इस आंदोलन में भाग लिया।
स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ
डॉ. हेडगेवार स्वतंत्रता के महत्व से भली-भांति परिचित थे। लेकिन एक मौलिक सवाल उन्हें अक्सर परेशान करता था। वह खुद से पूछते थे कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से भारत आए और इस राष्ट्र पर राज किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था, असंगठित था और उसमें कई सामाजिक बुराइयां थीं, जिसने अंग्रेजों के लिए भारत पर शासन करना संभव बना दिया।
उन्हें यह डर था कि यदि भारतीय समाज को मौलिक रूप से परिवर्तित नहीं किया गया तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी इतिहास खुद को दोहराता रहेगा। उन्होंने समाज को अधिक जागरूक, आत्म-गौरव से भरा हुआ और संगठित बनाने की आवश्यकता को समझा। उन्होंने हमेशा स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय गुणों वाले लोगों पर जोर दिया।
1930 में, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। इसके बाद, सभी संघचालकों की एक तीन दिवसीय बैठक हुई थी, जिसमें आरएसएस ने बिना शर्त आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया था। विभिन्न मुद्दों पर आरएसएस की अपनी नीति थी। नीति के अनुसार, डॉ. हेडगेवार ने सत्याग्रह में व्यक्तिगत क्षमता से आंदोलन में भाग लिया। उनके साथ उनके अन्य सहयोगी भी थे। यह नीति आरएसएस के काम को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी।
इस बात को ध्यान में रखते हुए, डॉ. हेडगेवार ने सरसंघचालक की जिम्मेदारी अपने लंबे समय के मित्र डॉ. परांजपे को सौंप दी। डॉ. हेडगेवार ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। लगभग हजारों लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया। वह वर्धा और यवतमाल होते हुए पुसद पहुंचे। जब वह सत्याग्रह के लिए पुसद पहुंचे तो हजारों लोग जमा हो गए थे। सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें नौ महीने की कैद हुई। जेल से रिहा होने के बाद डॉ. हेडगेवार ने सरसंघचालक की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा आरएसएस के काम के लिए समर्पित कर दी।
भारत छोड़ो आंदोलन और आरएसएस
अगस्त में, महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक में अंग्रेजों से ‘भारत छोड़ो’ कहा। अगले दिन से आंदोलन को गति मिली। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। विदर्भ क्षेत्र में बाओली (अमरावती), अष्टि (वर्धा) और चिमूर (चंद्रपुर) में आंदोलन देखा गया। चिमूर से खबरें बर्लिन रेडियो पर भी प्रसारित की गईं। यहां आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उद्धवराव कोरेकर और संघ के अधिकारियों दादा नाइक, बाबूराव बेगड़े, अन्नाजी सिरास ने किया। बालाजी राजापुरकर, एक आरएसएस स्वयंसेवक, ब्रिटिश गोलीबारी में मरने वाले एकमात्र आंदोलनकारी थे।
कांग्रेस के श्री तुकडोजी महाराज द्वारा स्थापित श्री गुरुदेव सेवा मंडल ने, संघ स्वयंसेवकों के साथ मिलकर चिमूर आंदोलन और सत्याग्रह का आयोजन किया था। चिमूर संघर्ष में, अनेक सत्याग्रहियों पर मुकदमा चलाया गया और अनगिनत स्वयंसेवकों को कैद किया गया। कई आरएसएस स्वयंसेवकों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।
उनमें से कुछ थे: राजस्थान में प्रचारक जयदेवजी पाठक, जो बाद में विद्या भारती में सक्रिय हुए; आर्वी (विदर्भ) में डॉ. अन्नासाहेब देशपांडे; जशपुर (छत्तीसगढ़) में रमाकांत केशव (बालासाहेब) देशपांडे, जिन्होंने बाद में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की; और श्री वसंतराव ओक जो बाद में दिल्ली के प्रांत प्रचारक बने। बिहार (पटना) में, प्रसिद्ध वकील कृष्ण वल्लभप्रसाद नारायण सिंह (बाबूजी) जो बाद में बिहार के संघचालक बने। दिल्ली में, श्री चंद्रकांत भारद्वाज, जिनके पैर में गोली लगी थी। इसके अलावा, कई आरएसएस स्वयंसेवक भूमिगत काम में शामिल थे। उदाहरण के लिए, अरुणा आसफ अली को दिल्ली में हंसराज गुप्ता ने शरण दी थी। महाराष्ट्र के सतारा के नाना पाटिल को पंडित सातावलेकर ने शरण दी थी, जो औंध के संघचालक थे।
आज़ादी के बाद भी औपनिवेशिक मानसिकता
राष्ट्र को यह विश्वास करने के लिए मजबूर किया गया है कि भारत केवल एक राजनीतिक इकाई है, मुख्य रूप से विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का समामेलन है। राष्ट्र को यह विश्वास करने के लिए मजबूर किया गया है कि स्वतंत्रता का श्रेय किसी विशेष विचारधारा और संगठन को जाता है। यह प्रचार है, इतिहास नहीं। यह प्रचार न केवल अनुचित है, बल्कि उन लोगों के साथ घोर अन्याय है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
स्वतंत्रता विभिन्न कारकों का संचयी प्रभाव है, जिसमें क्रांतिकारी तरीके, अहिंसक तरीके, आजाद हिंद फौज और सेना में विद्रोह शामिल हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड बहुत खराब स्थिति में था। वह पहले की तरह उपनिवेशों को चलाने में असमर्थ था। गौरतलब है कि भारत वह देश था, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष देखा। यह याद रखना चाहिए कि जिन उपनिवेशों में स्वतंत्रता संग्राम नहीं हुआ था, उन्हें भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता मिली। इसलिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने का श्रेय किसी विशेष संगठन, विचारधारा और आंदोलन को देना हास्यास्पद और अनुचित है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता के समय कहा था, “महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन का ब्रिटिश सरकार पर शून्य प्रभाव पड़ा है”। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और तत्कालीन बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल, पी.एम. चक्रवर्ती के अनुसार:
“जब मैं कार्यवाहक राज्यपाल था, लॉर्ड एटली, जिन्होंने भारत से ब्रिटिश शासन को हटाकर हमें स्वतंत्रता दी थी, भारत के अपने दौरे के दौरान कलकत्ता में राज्यपाल के महल में दो दिन रहे थे। उस समय, मैंने उनसे उन वास्तविक कारकों के बारे में लंबी चर्चा की थी, जिनके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। एटली से मेरा सीधा सवाल था कि चूंकि गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन काफी समय पहले ही समाप्त हो गया था और स्वतंत्रता के समय ऐसी कोई नई बाध्यकारी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, जिसके कारण अंग्रेजों को जल्दबाजी में जाना पड़े, तो उन्हें क्यों जाना पड़ा? अपने जवाब में एटली ने कई कारण बताए, जिनमें से मुख्य कारण नेताजी की सैन्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप भारतीय सेना और नौसेना कर्मियों के बीच ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी का क्षरण था। हमारी बातचीत के अंत में, मैंने एटली से पूछा कि गांधीजी का भारत छोड़ने वाली ब्रिटिश सरकार पर कितना प्रभाव था। सवाल सुनकर एटली के होंठ व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुड़ गए, और उन्होंने धीरे से कहा- न्यूनतम”।
‘स्व’ की भावना का पुनरुत्थान
भारत को अगस्त 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन हम ब्रिटिश या पश्चिमी विचारों से शासित होते रहे, जिनमें स्वतंत्रता की गहरी भावना का अभाव था। हमें 1947 में जो मिला वह केवल एक औपचारिक राजनीतिक स्वतंत्रता थी। हम ब्रिटिश और पश्चिमी विचारों की धारणा से सोचते थे। हमारे देश की राजनीतिक शब्दावली भी ब्रिटिश या पश्चिमी दर्शन से निर्णायक रूप से प्रभावित थी। हम खुद को ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ के अनुयायी कहते थे, जिसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। हमने उस शिक्षा प्रणाली को जारी रखा, जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा शुरू किया गया था। हम उन कानूनों के साथ जारी रहे, जिन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा उनके एजेंडे के अनुरूप बनाया गया था।
हमारा राष्ट्र ‘स्वतंत्रता’ का वास्तविक अर्थ भूल गया था या उसे भुला दिया गया था, जिसका अर्थ है सभी प्रकार की गुलामी से मुक्ति। 1947 के बाद बौद्धिक स्वतंत्रता की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निहित स्वार्थों द्वारा राष्ट्र को ‘स्व’ की भावना को भुला दिया गया। इसी वजह से लोग व्यंगात्मक रूप से कहते थे कि ‘भारत’ पर ‘काले अंग्रेजों’ का शासन है।
गुलामी कभी भी केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं होती है, बल्कि यह मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक – बौद्धिक और भावनात्मक – मन की स्थिति होती है। गुलामी किसी व्यक्ति और बड़े पैमाने पर समाज की प्रेरणा और कार्यों को बुरी तरह प्रभावित करती है। वास्तव में, गुलामी व्यक्ति को स्वतंत्रता के बारे में भूलने पर मजबूर कर देती है। स्वतंत्रता के अभाव में, किसी व्यक्ति और समाज का विकास केवल रुकता नहीं है, बल्कि प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा बन जाता है।
औपनिवेशिक नीतियों और मानसिकता को जारी रखने के परिणामस्वरूप गंभीर समस्याएं हुईं क्योंकि ब्रिटिश नीतियां मूल रूप से उनके अपने शासन के लिए बनाई गई थीं, न कि भारत के लिए। उदाहरण के लिए, राजनीतिक दलों ने ब्रिटिश ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति का पालन करना जारी रखा। इसने आर्य और द्रविड़ या शैव और वैष्णव जैसे सतही आंतरिक संघर्षों को बढ़ावा दिया। ये नीतियां ब्रिटिश शिक्षा पर आधारित थीं, जिसका उद्देश्य जाति और भाषा जैसी विभिन्न रेखाओं के साथ हिंदुओं को विभाजित करना था। यह विचारधारा मानती थी कि भारत का अस्तित्व 1947 में हुआ था और इस राष्ट्र के प्राचीन और शाश्वत अस्तित्व को नकारती थी।
हालांकि, हमारे पास परिदृश्य में बदलाव के कुछ सकारात्मक और उत्साहजनक संकेत हैं। हमारे पास ऐसी कई घटनाएं हैं, जिनमें हम लोगों की मानसिकता/रवैया/विचारधारा में बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। लोग अब आत्म-जागरूक हो गए हैं। लोग जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन गए हैं, जो चौतरफा प्रगति के लिए बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। भारत के लोगों में अलगाव की भावना विकसित हो गई थी क्योंकि वे ‘स्व’ से अवगत नहीं थे। अब अलगाव को ‘अपनेपन’ की भावना से बदल दिया गया है।
नए संसद भवन के मामले को लीजिए, जो भारत के सांस्कृतिक एकीकरण के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। यह अपनी जीवंतता, एकता और शाश्वत मानवीय मूल्यों को शामिल करते हुए समृद्ध भारतीय विरासत का एक प्रदर्शन है। संसद में रखा गया सेंगोल, निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और सीमाओं की याद दिलाता है। दूसरी ओर, पुराना संसद भवन एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में बनाया गया था, जो औपनिवेशिक शासन और गुलामी का प्रमाण था।
‘स्व’ की भावना को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जो देश में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करेगी।
यह नई ऊर्जा राष्ट्र के जीवन के सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होगी, जिसमें भौतिक प्रगति भी शामिल है। यह आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान प्राचीन भारतीय मूल्यों का उपहास या अपमान करके कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन राष्ट्र सभी हमलों और आक्रमणों के बावजूद प्राचीन मूल्य प्रणाली के कारण ही जीवित रहा। भारतीय मूल्यों पर जोर देना ही वास्तविक स्वतंत्रता है, जिसमें औपनिवेशिक विचारों और रवैये के लिए कोई जगह नहीं है।
