सदाशिव-लक्ष्मीबाई दम्पत्ति का आठवां अपत्य युगाब्द 5007 माघ कृष्ण एकादशी (उत्तर में पौष) मूल नक्षत्र में तदनुसार सन 19 फरवरी 1906 को, सोमवार ब्रह्म मुहूर्त पर नागपुर में मामाजी आबा रायकर के घर में जन्म हुआ। तिथि, नक्षत्र आदि देखकर उस पुत्र का नाम माधव रखा गया।
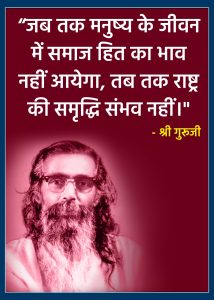
माधव की प्राथमिक शिक्षा रायपुर, चंद्रपुर, भण्डारा और खण्डवा में हुई थी। प्रत्येक कक्षा में वह अग्रगण्य छात्रों में एक था। अध्यापक के प्रश्नों के तत्काल उत्तर देने के लिए वह न केवल उत्साही, अपितु सक्षम भी थे । इसलिए जानकार छात्रों की प्रकृति के अनुसार वह हमेशा अगुआ थे।
इसी कालखंड में, जब मधु की आयु 11 की हुई तो ताई-भाऊजी ने उसके उपनयन की योजना बनाई। 1919 में मधु ने अंग्रेजी हाईस्कूल में प्रवेश किया। सातवीं के बाद हाईस्कूल एंट्रेंस एंड स्कालरशिप की परीक्षा में जीतने पर उनको प्रतिमास 4 रूपये की छात्रवृति प्राप्त हुई।
बचपन से ही माधव को पढ़ना बहुत पसंद था। उनका मन पढ़ने में खूब लगता था। पढाई के साथ –साथ वे खेलकूद में भी भाग लेते थे और हाँकी उनका प्रिय खेल था।
1922 का वर्ष नवतरुण माधव के सामने शिक्षा निर्धारण का महत्त्वपूर्ण समय था। भाऊजी अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने इसी दिशा में प्रयास करते हुए पुणे के महाविद्यालय से आवेदन पत्र मंगवाया और भरकर भेज दिया। अपेक्षानुसार माधव को इस महाविद्यालय में प्रवेश मिला । किंतु बीच में एक बाधा आ गई। एक नया प्रावधान आया कि प्रदेश की संस्थाओं में स्थानीय छात्रों को ही प्रवेश मिल सकता है। उसके अनुसार मुंबई प्रेसीडेंसी के महाविद्यालय में सेंट्रल प्रोविंस का छात्र अयोग्य ठहरा। इस कारण माधव का प्रवेश रद्द हुआ और उनको हतास होकर नागपुर लौटना पड़ा। उन्होंने वहाँ के हिस्लाप महाविद्यालय में प्राणिशास्त्र के विज्ञान विभाग में प्रवेश लिया।
नागपुर शिक्षण के दौरान माधव ज्ञान की अन्य कलाओं के प्रति भी रूचि लेने लगे। सुप्रसिद्ध मुरली वादक पंडित सांवलाराम के सम्पर्क में आकर उनसे मुरली सीखने लगे। निरंतर अभ्यास से माधव ने संगीत के कई रागों पर अच्छी पकड़ बना ली।
काशी नगरी का गोलवलकर जी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। माधव गोलवलकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने यहीं आए और 1924 में प्राणिशास्त्र की बी.एस.सी. में प्रविष्ट हुए। ब्रोचा होस्टल के 301 कमरे में उनका ठिकाना बना।
काशी उनके दिव्य जीवन दर्शन का प्रधान केंद्र था। ऐनी बेसंट ने वहाँ सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज प्रारंभ किया था और बाद में महामना मालवीय जी की प्रार्थना को मानते हुए उसे हिन्दू विश्वविद्यालय में विलीन किया गया था। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में दिव्य जीवन संघ प्रतिष्ठित माना जाता था। उस प्रभावी वातावरण में गोलवलकर उसके सम्पर्क में आए और प्रमुखों की प्रेरणा से उन्होंने उस दर्शन का अध्ययन भी किया।
1928 के जून में ज्येष्ठ प्राध्यापकों एवं पूज्य पिताजी से परामर्श करके माधवराव गोलवलकर चेन्नई के मत्स्यालय में जलचर सम्बन्धी अनुसंधान के लिए पहुंचे। ट्रिप्लिकेन के एक कमरें में वे किरायेदार थे। पिताजी उनको मर्यादित आमदनी से 50 रूपये भेजते थे। उसके अनुसार उन्होंने अपना कामकाज संभाला। मत्स्यालय बहुत दूर नहीं था इसलिए वे वहाँ पैदल ही चलकर जाया करते थे। चेन्नई में भी गोलवलकर को अच्छे दोस्त मिले।
उस समय का एक अनुभव उन्होंने स्वयं बताया ‘मद्रास मत्स्यालय में अध्ययन के दौरान हम कुछ विद्यार्थी समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। एक बार एक नाव में हम सब बैठे थे । मैं अपने दोनों पैर पानी में डाले बैठा था। हमारी नाव के समीप एक दूसरी नाव भी थी। एकाएक उस नाव का एक नाविक तमिल भाषा में जोर से चिल्लाया। मुझे तो उसका चिल्लाना समझ में नहीं आया। परंतु जो साथ में थे उन्होंने तुरंत मुझे पैर ऊपर कर लेने को कहा । मैंने पैर ऊपर कर लिए। नीचे पानी में देखा तो शार्क मछली नाव तक आ पहुंची थी।’ शार्क मछली का इतनी तेज गति से आना, दूर से नाविक का उसे पहचानना, फिर तुरंत सतर्क करने के लिए चिल्लाना, खाने से वंचित होते ही मुँह पीछेकर वापस जाना आदि स्नातकोत्तर छात्रों के लिए नया अनुभव था। शायद वह भी उनके अनुसंधान में सहायक हुआ होगा।
1929 के मध्य में चेन्नई का अनुसन्धान अधूरा छोड़कर माधवराव नागपुर आये। दो साल बाद, 1931 में काशी विश्वविद्यालय में अध्यापक बने। बीच का यह अंतराल उन्होंने नागपुर में मामा रायकर के यहाँ रह कर बिताया।
माधवराव गोलवलकर का संघप्रवेश 1931 में हुआ था जब वे काशी में अध्यापन के लिए आये थे । उससे पूर्व नागपुर में उनके कई मित्र एवं परिचित संघ के स्वयंसेवक थे।
विश्वविद्यालय में गुरूजी 16 अगस्त 1931 को आए। उसके तुरंत पश्चात 29 अगस्त 1931 को महामना मालवीय जी गोल-मेज सम्मेलन के लिए लन्दन रवाना हुए। साढ़े चार महीने बाद 14 जनवरी 1932 को वापस आए। इसी अंतराल में विश्वविद्यालय में संघशाखा का आरम्भ हुआ था । प्रत्यागमन के बाद पूज्य मालवीय जी को अल्प सा अवकाश मिलने पर गुरूजी ने संघ के कार्यकर्ताओं के साथ उनके दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
स्वभाव और व्यक्तित्व
आदत मानव का मानक है। आदतों से भी व्यक्ति का आकलन सम्भव है। जैसे आदतें जमकर स्वभाव बन जाती हैं वैसे ही स्वभाव आदतों को भी पैदा करता है। एक व्यक्ति के नाते गुरुजी की कई आदतें थीं जो उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाती हैं :-
गुरु जी की भाषण शैली प्राध्यापक की थी। एक प्रांत में पहुँचने पर प्रांतीय भाषा में सम्बोधन करने की और दो वाक्य प्रांतीय भाषा में बोलने की। भाषण के प्रारम्भ में उनकी आव़ाज बहुत नीचे की होती, दो तीन मिनट के बाद मध्यम स्वर में आ जाती। बाद में भाषण बिना उतार-चढ़ाव के धाराप्रवाह आगे बढ़ता। भाषण में जिस प्रसंग का उल्लेख आता उस सम्बन्धित व्यक्ति का नाम वे कभी नहीं बताते, ‘एक प्रसिद्ध कवि, एक बड़ा नेता’ इस प्रकार के संकेत जरुर देते। इससे व्यक्ति विशेष के बारे में सामान्य स्वयंसेवक पूर्वग्रह से मुक्त रहता। हिंदी, मराठी और अंग्रेजी वे एक ही प्रकार से बोलते थे। अधिकतर 50- 60 मिनट के अन्दर उनका भाषण पूरा हो जाता था।
गुरूजी की बैठक शैली उनकी भाषण कला से बिल्कुल भिन्न थी। उनकी बैठक सत्संग की सम्वाद शैली के समान थी जिसमें विनोद, पूछताछ, टीका-टिप्पणी आदि से वे कार्य का आकलन करते और कार्यकर्ता को परखते समझते।
गुरूजी समय के बहुत पाबन्द थे। अतः संघ के या अन्य किसी भी निर्धारित कार्यक्रम में ठीक समय पर जाना उनकी आदत थी । गुरूजी केवल स्वदेशी कपड़ों का उपयोग किया करते थे।
गुरूजी स्वयंसेवकों को राम, गोविन्द जैसे नाम अथवा बाबा बापू जैसे घरेलू नामों से पुकारते थे । त्रिवेदी, तिवारी जैसे जातिवाचक नामों से नहीं। इससे स्वयंसेवक गुरूजी के साथ एक आत्मीयता का अनुभव भी किया करते थे।
गुरूजी का जीवन बहुत पारदर्शी था, जैसे चन्दन की सुगंध उजाले और अँधेरे में एक समान होती है उसी प्रकार उनका एकांत अथवा अनेकांत बिना भेद एक ही था।
डॉ. हेडगेवार के सहवास में
1932 की गर्मी की छुट्टियों में गुरूजी नागपुर आए। उसी काल में उनका डॉ. हेडगेवार से प्रथम मिलन हुआ। मामा रायकर के घर से कहीं पर जाते समय उन्होंने इधर की दिशा में आ रहे डॉक्टर जी को देखा। डॉक्टर जी सीधा उनके सामने खड़े हुए और पूछा ‘आप हैं क्या माधवराव गोलवलकर?’ यह था उनका डॉ. हेडगेवार के साथ प्रथम परिचय।
नागपुर में डॉक्टरजी के घर पर गुरूजी नियमित आने लगे। संघ की शाखा में भी वे नियमित उपस्थित होने लगे। लाहौर के वर्ग में डॉक्टरजी का कमर दर्द अधिक हो गया। अतः आगे के कार्यक्रम स्थगित कर वे दिल्ली होकर सितम्बर को नागपुर वापस आए। बीस दिन लंबे उस प्रवास में डॉक्टरजी को निकट से गुरूजी का निरीक्षण करने का और गढ़ने का पर्याप्त अवसर मिला।
आह्वान और विस्तार
1940 के नागपुर संघ शिक्षा वर्ग में संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने कृतार्थ होकर कहा था ‘आज मैं मेरे सामने भारत का लघुरूप देख रहा हूँ।’ 1938 से एक ओर वे गुरूजी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को गढ़ रहे थे, दूसरी ओर शिक्षाग्रहण और संघकार्य, दोनों एक साथ करने के लिए भाऊराव देवरस को लखनऊ, राजभाऊ पातुकर को लाहौर, कृष्ण जोशी को सियालकोट, मोरेश्वर मुंजे को रावलपिंडी भेजा था । पूर्ण कालीन कार्यकर्ता के नाते वसंतराव ओक को दिल्ली, नरहरि पारखी को बिहार, बापु दिवाकर को पटना, विठ्ठलराव पत्की को बंगाल, गोपालराव येरकुंटवार को मुंबई भेजा था। इसके अतिरिक्त यथाकाल यथास्थान प्रवास के लिए वे दादाजी परमार्थ और बाबासाहेब आपटे को भेजा करते थे। इस प्रकार संघ कार्य देशभर में फैलाने के लिए योजनाबद्ध कार्य किए गए थे। यह थी गुरूजी की पूंजी जब वे सरसंघचालाक बने।
हिंदवः सोदराः सर्वे
1961 का वर्ष गुरूजी के जीवन में सामाजिक समरसता की दृष्टि से विशेष स्मरणीय है। 1 जनवरी को पुणे में दैनिक नवाकाल के संपादक ने गुरूजी का साक्षात्कार लिया। अल्पसंख्यकों की समस्या, परावर्तित लोगों के शुद्धिकरणविधि, वैज्ञानिक युग में काल ब्रह्म रुढियों को बदल देने की आवश्यकता आदि विषयों पर गुरूजी का मत ग्रहण कर उन्होंने पूछा ‘ हिन्दू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, क्या उसमें परिवर्तन जरुरी नहीं है? गुरूजी का उत्तर ध्यान देने लायक है।
- शहरों से लेकर ग्रामीण भागों तक और गिरी-कंदरों से लेकर मैदानों तक फैले हुए हिन्दू समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जाति-पाति, गरीबी, अमीरी, साक्षर, निरक्षर, विद्वान् आदि का विचार न करते हुए सबको एकत्र लाना, यही संघ का कार्य है।
- मेरा यह अभिप्राय नहीं था कि अपने समाज में कुछ अस्प्रश्य हैं। संघ में स्प्रश्यता –अस्प्रस्यता क विचार ही नहीं होता, यह बताने की आवश्यकता नहीं है।
- हरिजन बांधवों को अगर आज की परिस्थिति से क्षोभ है, तो इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। उनके मन की कटुता दूर हो और वे अपने को समाज का गौरवपूर्ण संग समझें, इस पद्धति से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए।
- युगानुसार स्नाज के व्यवहार परिवर्तन होता रहता है। कानून को परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ता है और निरुपयोगी सिद्ध हुआ तो रद्द करना पड़ता है, यह सदैव का अनुभव है। उसमें महत्त्व की बात यह है कि परिवर्तन करते समय मूल परंपरा का सूत्र खंडित नहीं होना चाहिए।
समाज की वर्तमान अवस्था के संबंध में उन्होंने कहा “हम भूल गए कि हमें संगठित सामाजिक इकाई के रूप में जीना है। अपनी विशाल मानवशक्ति को भूलकर हम एकांतिक बन गए थे। कुछ व्यक्ति संदेह करते हैं कि इतनी जातियों, सम्प्रदायों, उपजातियों, भाषाओं, रीति-रिवाजों, पहनावों, भोजनों आदि की विभिन्नताओं के रहते हुए क्या हमारे समाज का संगठित रूप में खड़ा होना संभव है ? किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपरी विभिन्नताओं के बीच भी एक आंतरिक एकता की सलिला हमारे बीच प्रवाहमान है”।
यह जानकारी माननीय रंगाहरि जी द्वारा लिखित ‘गुरुजी गोलवलकर जीवन चरित्र’ पर आधारित है।
